मैंने धर्म की बुराइयों पर लिखना क्यों और कैसे शुरू किया- शेष नाथ वर्णवाल

मेरे मित्रों और जान-पहचान वालों को शिकायत है कि मैं धर्म पर इतना क्यों लिखता हूं? धर्म से क्यों इतनी शिकायत है? ..तो साथियों आज मैं अपनी कहानी यहां रख रहा हूं। बचपन से मैं ऐसा नहीं था। जब छोटा था, तब सोचता था कि ईश्वर का अस्तित्व सचमुच में होता है। नहीं तो पूरी दुनिया, पूरा समाज क्यों उसको मानता? ईश्वर को खुश करने या उसकी उपासना करना भी तब सही प्रतीत होता था। पर तब ईश्वर के बारे में, मेरा न तो कोई व्यक्तिगत अनुभव था और ना ही उसके बारे में कोई खास समझ। बस देखा-देखी का विश्वास था। चूंकि ईश्वर में विश्वास था (देखा-देखी वाला ही), तो उसकी उपासना भी ज़रूरी समझता था।
सर्वशक्तिमान ईश्वर को खुश करने से बहुत फायदे हो सकने की सम्भावना थी, साथ ही साथ डर भी था। ईश्वर से भी और भूत-पिशाच आदि से। रात में कहीं अकेला जाता था,तो हनुमान चालीसा पढता था। खासकर, “भूत-पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे”, वाली लाईन। तब से आज तक ना तो कोई भूत मिला, ना ही ईश्वर।
स्कूल के दिनों में और फिर कॉलेज के दिनों में भी, विवेकानन्द, गांधी, ओशो आदि को पढ़ने की आदत लग गई। धीरे-धीरे समझ में आया कि किसी चीज़ को मानने के लिए जानना ज़रूरी है। अपने अनुभव के बिना क्या पता जिस चीज़ को देखा-देखी में मान रहे हैं, सच में वो चीज़ हो ही नहीं। तो संदेह की शुरूआत हो चुकी थी। बाद में यह भी तर्क सही लगा, कि जो व्यक्ति बिना जाने मान लेता है उसके जानने की सम्भावना ही खत्म हो जाती है। उसका सवाल करना, उसकी कौतुहलता और उसकी अज्ञानता ही जानने तथा अनुभव करने की शर्त है। हम तर्क और जिज्ञासा को मार कर, भला कैसे ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं?
पता नहीं कैसे मुझमें तर्क का विकास होता चला गया और ढूंढने की प्रवृति बढ़ती गयी। मेरे घर में एक गुरुजी को मानते थे, (अब भी मानते हैं), वो जीवन और मनुष्य की बात अच्छा करते थे, पर मुझे पसंद नहीं आये। उनकी विलासिता और अकूत सम्पति के बारे में मन में आता था कि यदि वे उतने मानव के बारे में सोचते हैं, तो उस धन को क्यों नहीं उनके कल्याण में लगा देते? क्यों विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं? उनको यह गुरु का पद भी अपने पिता से मिला था, तो मैं सोचता था कि क्या यह वंशानुगत होता है?
इसके अतिरिक्त धर्म और ईश्वर के बारे में, मैं बहुत ही कुतूहल अपने भीतर पाता था, जैसे बाबा लोग कहते हैं न कि जीवन सफल करना है, वैसा ही। ईश्वर और धर्म के इस कौतूहल में रामकृष्ण मिशन रांची को पत्र लिखने को मजबूर किया, फिर जवाब भी आया। आना-जाना जारी रहा और आखिर में रामकृष्ण मिशन से दीक्षा ले लिया। गुरु और मंत्र दोनों मिला। हालांकि तब भी मैं उपासक था और मैं सन्यासी बनना चाहता था, पर वहां के प्रमुख स्वामी शशांकानंद जी ने कहा, “पढ़ाई पूरी करके आओ, तब कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाएगी।” इस दौरान उनके आश्रम में, करीब एक महीने रहा। उनकी दिनचर्या और समाज के प्रति नज़रिया देखकर मैं बहुत प्रभावित नहीं हुआ।
मैं तो अपना सबकुछ छोड़कर संन्यासी बनना चाहता था और मानवता के लिए कुछ अलग करना चाहता था। शायद विवेकानन्द की पुस्तकों को पढ़ने का असर था। तब लोगों की दुर्दशा और गरीबी पर मैंने स्वामी जी से कुछ सवाल उठाये और संन्यासी बनने के बारे में, अपनी भूमिका के बारे पूछा। उन्होंने तब कहा था, “रामकृष्ण मिशन एक मशीन है और तुम्हें एक पुर्जे की तरह इसमें फीट होना है, अपनी सोच के अनुसार तुम यहां काम नहीं कर सकते।” इस कथन से मुझे बहुत दुःख और निराशा हुई। मैं इंसान था और मशीन बनने को तैयार नहीं था। बहुत जल्द ही मेरा, वहां से मोह भंग हो चुका था।
फिर धर्म और अध्यात्म की जिज्ञासा में, दिल्ली में निरंकारी बाबा के पास गया, आशाराम को भी मानने लगा, ओशो ध्यान भी किया और पता नहीं क्या-क्या किया। कई प्रकार की किताबें पढ़ने लगा और भक्ति-ध्यान करने लगा, पर ऐसा कोई ज्ञान या अनुभव नहीं मिला, जिसे ईश्वरीय अथवा सत्य का साक्षात्कार जैसा कुछ कह पाता। हालाँकि ध्यान में विचारहीन हुआ कुछ बार। यह अनुभव अच्छा था, पर ना ही ईश्वरीय अथवा सत्य जैसा कुछ।
फिर इसी दौरान ही मन नहीं माना, तो एक बार सोचा बोधगया पास है, वहां जाकर कुछ देखता हूं। फिर बोधगया गया, तो पता चला कि विपश्यना नामक एक ध्यान वहां करवाया जाता है। मैंने वहां के व्यवस्थापक से कहा कि मुझे विपश्यना करना है। उन्होंने कहा, विपश्यना शिविर अभी खत्म हो गया, अगली बार आना, तारीख भी बताया। मैं वापस घर (कोडरमा जिला, तब बिहार) लौट गया। फिर तय समय पर विपश्यना के लिए आया और 10 दिनों के लिए विपश्यना शिविर में भाग लिया। इस शिविर का अनुभव अच्छा रहा; ईश्वरीय नहीं, बल्कि मानवीय रहा। वो विपश्यना में, अपनी शरीर की संवेदना को महसूस करना सीखाते हैं। मुझे महसूस हुआ कि जो चेतना मुझमें है, वही चेतना अन्य मनुष्यों, जंतुओं और पेड़-पौधों में भी है। उस दिन मैं बहुत रोया। मैंने सोचा और महसूस किया कि कितना स्वार्थी था मैं। खुद का दायरा कितना सीमित था।
इस घटना (विपश्यना) के बाद कभी ईश्वर की तलाश नहीं की। न ही पूजा-उपासना की। बल्कि मैं अपने तर्कों में और भी दृढ हो गया और इंसानियत में विश्वास करने लगा था। मेरे लिए इंसान और पृथ्वी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गये।
मेरे बचपन की एक याद भी भी इससे जुड़ी है। वह है अयोध्या का राम-मन्दिर और बाबरी-मस्जिद का विवाद, हिन्दू-मुस्लिम के झगड़े, एक धर्म के लोगों का दूसरे के प्रति घृणा। इसने भी मुझे धर्म से दूर किया। अगर धर्म अच्छा था, तो धर्म को मानने वाले लोगों को ज़्यादा मानवीय होना चाहिए था। बल्कि अनुभव और जानकारी में, सच इसके विपरीत था। मेरे पिता जी खुद को एक कट्टर हिन्दू कहना पसन्द करते थे, जो मुझे नापसंद था। हालांकि मेरी मां बहुत ही उदार थी और सभी धर्मों और जातियों के घरों में आना-जाना तथा मेलजोल करती थी। वह छुआछुत नहीं मानती थी। मैं माँ से प्रेरित था।
अपने आसपास, मुझे यह भी अनुभव हुआ, कि जो खुद को धार्मिक कहते हैं, वही जाति-भेद भी मानते हैं। दहेज़ भी लेते हैं। बहुओं की दहेज़ के लिए हत्या तक कर देते हैं। पति-पत्नी के सम्बन्ध मानवीय नहीं, बल्कि मालिक और दासी जैसा है। पुरुष खाने के वक्त पानी तक नहीं लाता, थाली में ही हाथ भी धोता है। एक महिला के लिए ऐसा कल्पना करना भी, असंभव था।
इन सब चीज़ों को देखकर, तब मैं सोचता था, ये कैसे धार्मिक लोग हैं, जो अपने भोज में महार, भुईयां, घटवार, पासवान आदि लोगों को एक साथ बैठ कर खाने नहीं देते। बात सिर्फ हिन्दू धर्म की नहीं थी। अपने मुस्लिम दोस्तों से बात करके भी धार्मिक कट्टरता का अहसास हुआ। ऐसा लगा कि धर्म के मामले में, वे बात करने से कतराते हैं, आलोचना और सवाल खड़ा करना तो बहुत दूर की बात है। लड़कियों के पहने बुरके से भी मैं सोच में पड़ जाता। मेरे कुछ मित्र कहते थे यह वह मर्ज़ी से करती हैं। मेरा सवाल होता था, सभी लोग? वो भी बचपन से।
उस दौरान मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली में बाल अधिकार में पीजी डिप्लोमा कर रहा था। कुछ दिन नेहरु विहार में रहा, फिर रोज आने जाने में दिक्कत होने के कारण बटला हाउस में रहने लगा था, जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही रहते थे। बात 2008 की थी। मैं और मेरा एक मुस्लिम सहपाठी साथ रहते थे और खुद से खाना बनाते थे। कई बार खाना बनाने का मन नहीं होता था, तो आसपास के होटल (ढाबा जैसा) में जाकर खाना खा लेता था। सभी होटल मुस्लिमों के थे, तब भी खाता था। मुझे यह भी जानकारी थी कि कई होटल में गाय का मीट भी बनाते हैं, और सब्जी तो गिने-चुने लोग बनाते हैं। तब भी खाता था। हालांकि मैं बचपन से शाकाहारी रहा था, फिर भी मुझमें यह तर्क आ गया था कि अगर बकरा खाना गलत नहीं है, तो गाय खाना भी गलत नहीं हो सकता। अगर एक जीव की हत्या पाप नहीं है, तो दूसरे जीव की हत्या भला पाप कैसे हो सकता है? हालांकि अबतक मैं शाकाहारी ही रह गया हूं। वैसे इस शाकाहारी होने में, मेरा कोई खास योगदान नहीं है, माँ-बाप और परिवार से ही मिला है यह।
कुछ और दिन बीते, अब अकसर मेरे घर में, मित्रों से और अन्य कई लोगों से धर्म को लेकर बहस, नोक-झोंक, विवाद होने लगे थे। उनके तर्क से मैं सन्तुष्ट नहीं होता था और मेरे तर्कों का उचित जवाब वो देते नहीं थे।
मुझे यह तय हो गया कि धर्म जो कहने को मानवता, प्रकृति का नियम, कर्त्तव्य या जो धारण करने की परिभाषा में समेटा जाता है, वैसा नहीं है। बल्कि व्यवहार में, इसका रूप बहुत ही कुत्सित है। धर्म लोगों में भेद पैदा करता है और लोगों को अन्धविश्वासी बनाता है। हर धर्म के लोग अपने धर्म को दूसरे के धर्म से बेहतर साबित करने कि चेष्टा करते हैं। अलग अलग उपासना स्थल जाते हैं, एक नहीं।
धर्म के नाम पर राजनीति भी समझ आने लगी थी। जिस बाबरी ध्वंश के समय, बच्चा होने के बावजूद, मैं अपने पिताजी के साथ छोटा-सा तलवार लेकर अपने धार्मिक समुदाय के जुलूस में शक्ति प्रदर्शन करने गया था, अब उसकी जड़ में सत्ता का खेल समझ में आने लगा। मुझे लगा धर्म तो हथियार है सत्ता हासिल करने का। यह सत्ता समाजिक संबंधों में भी दिखने लगा और राजनीति में भी।
मुझे अब धर्म को बेनकाब करना था। इसलिए बाईबिल, भागवत गीता, कुरान आदि पढ़ने लगा। बटला हाउस में रहते हुए, मेरे एक मुस्लिम मित्र (रूममेट नहीं) को आपति हो गई कि मैंने उनके पवित्र कुरान को और दूसरे किताबों के बीच ऐसे ही कैसे रखा है? उसके हिसाब से मुझे उसके पवित्र कुरान को अलग से ईज्जत देनी थी, जो मैं नहीं करता था। मेरे लिए वह एक किताब थी, कोई पवित्र चीज़ नहीं। हालांकि यह मेरी खरीदी हुई पुस्तक थी, पर मैं अपने दूसरे किताबों के साथ उसे नहीं रख सकता था। झगड़े के बाद, यहांं भी धार्मिक कट्टरता का अनुभव हुआ। उसके पहले हम बड़े अच्छे मित्र थे। अब नहीं रहे। कभी नहीं रहे। ऐसे कई अनुभव धर्म के नाम पर होते रहे।
मैंने तय किया कि मैं किसी भी धर्म के साथ खुद को नहीं जोडूंगा, जाति भेद नहीं मानूंगा और अपने विवाह में दहेज़ नहीं लूंगा। घर वालों की लाख मिन्नतों और नाराज़गी के बावजूद मैंने अंतरजातीय विवाह किया, दहेज़ भी नहीं लिया। मेरे लिए धर्म और जाति दो सबसे बड़े चुनौती बन गए। हर वो परम्परा और व्यवस्था का व्यक्तिगत जीवन में विरोध करना शुरू किया जो धर्म के नाम पर, झूठे पारिवारिक सम्मान के नाम पर जारी है और शोषणपरक है। भगत सिंह की पुस्तिका ‘मैं नास्तिक क्यों हूं’ पढ़ने के बाद धीरे-धीरे मैं खुद को नास्तिक भी समझने लगा, जो परम्परा को जांचने की बात करता है।
पहले ही स्टीफन हाकिंग, नीत्से, मार्क्स, पाओलो फ्रेरे आदि को पढ़ चुका था, अब धीरे धीरे यह अहसास हुआ कि मैं अकेला ऐसा सोचने वाला नहीं हूं, बल्कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत विश्वास आया खुद में और खुद की बात को बिना डरे व्यक्त करने का साहस करने लगा।
आखिरी घटना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल फरवरी या मार्च (2017) का है, जैसा कि मेरी फिल्मों को देखने की आदत है (खुद को फिल्मची तक कहता हूं) ), एक फिल्म देख रहा था (कंप्यूटर पर)। फिल्म का नाम था पिन्जर। भारत-पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी पर चंद्रप्रकाश द्विवेदी की यह फिल्म देखी, तो सन्न रह गया (पूर्व में, कुछ ऐसा ही असर तस्लीमा नसरीन की पुस्तक ‘लज्जा’ पढ़ कर भी हुआ था)। रात भर सो नहीं पाया। बहुत रोया। मैंने सोचा, “यह धर्म ही है, जो इतने लोगों की हत्याओं का कारण है।” “इतनी घृणा मानवता से, सिर्फ धर्म के ठप्पे के कारण?” “ऐसा ठप्पा जिसे हमारे माँ-बाप और समाज द्वारा हमारे ऊपर लगा दिया जाता है, जब हम अबोध होते हैं।” ऐसे धर्म पर कैसा गर्व जिसे हमने खुद अर्जित नहीं किया, अपने विवेक से नहीं अपनाया, बस हिन्दू के घर में जन्म हो गया, तो हिन्दू हो गए। मुसलमान के घर में जन्म हो गया, मुसलमान हो गए।
उसी रात मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन में धर्म के नाम पर समाज में व्याप्त कट्टरता, कठमुल्लावाद, अंधभक्ति और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ विरोध करूंगा और मानवता के लिए जो ठीक लगेगा, उसे ही मानूंगा। मुझे अहसास हो गया कि धर्म, जाति, कुरीति, अंधश्रद्धा आदि पर समाज में बहस का माहौल नहीं होने से कट्टरता और मूढ़ता और भी बढ़ती है। इसलिए इनपर खुलकर बात करना ज़रूरी है। इसके लिए उसी रात मैंने एक ब्लॉग शुरू किया – गो अथीस्ट (अब www.goatheist.in) और लिखना शुरू किया।
उस दिन से अब कोई एक साल हो गया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि तर्क और सवाल करने वाले लोगों से हर धर्म-सम्प्रदाय के लोगों को क्यों खतरा रहता है? वे नहीं चाहते कि कोई पीढ़ी सोचने समझने वाली और तर्क करने वाली पैदा हो। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि सोचने समझने वाले व्यक्ति को कंट्रोल करना असान नहीं होता, वह देर सबेर अपनी दृष्टि दुनिया और समाज के प्रति विकसित कर ही लेता है। उसे गुलाम बनाना आसान नहीं होता। अपनी ज़बरदस्ती की सत्ता थोपना आसान नहीं होता। वह गलत और संशय प्रतीत होने पर आपसे सवाल पूछ सकता है। आपके विचार से अलग एक विकल्प सुझा सकता है। आप विचार और कार्यों कि आलोचना कर सकता है। आप नहीं सुधरे तो आपका विरोध भी कर सकता है। तो तर्क और सोचने-समझने के बड़े खतरे हैं, उनके लिए, जो चाहते हैं सत्ता उन्हीं के पास रहे। धन और दबंगई उनके पास ही रहे। धर्म, पितृसत्ता और जाति भी तो एक प्रकार का सत्ता ही है।
हमारी सोचने-समझने और तर्क की परिणति इतने तक ही पहुंचती तब तो ठीक था, पर तर्क करने वाला और सोचने वाला व्यक्ति सरकार के कार्यों की समीक्षा कर सकता है। उसके नाकारापन को जनता के सामने ला सकता है। आदिवासी इलाकों में पूंजीपति-दलालों के हाथ बेचे जा रहे प्राकृतिक संसाधनों की पोल खोल सकता है। पण्डे, मौलवियों के ईश्वर, अंधविश्वास और ग ढोंग पर भी आपको आईना दिखा सकता है। इसलिए बहुत से खतरे हैं, सोचने-समझने और तर्क करने के।
इसीलिए न सरकार चाहती है कि लोग अपनी सोच को वैज्ञानिक और तर्क से पुष्ट करें और न धर्म के ठेकेदार। यही कारण है कि बहुसंख्य जनता उन्हें अपना माई-बाप मानती रहती है और ढ़ोंग, आडम्बर, लूट, उत्पीड़न, भक्ति, मूढ़ता, भ्रष्टाचार आदि जारी रहता है और हम भारत-पाकिस्तान, गाय-सूअर, सचिन-धोनी और सास-बहू में उलझे रहते हैं। वे चाहते हैं, स्थिति ऐसी ही बनी रहे। लोग जागरूक न बनें, वरना धर्म, पाकिस्तान, हिन्दू-मुस्लिम की जगह विकास, शिक्षा, सवास्थ्य आदि मुद्दे राजनीति के गलियारों में सुने जाते।
इस तरह से, इन सब अनुभवों से गुज़र कर, सोचने-समझने के बाद, मैं अब अपने संकल्प पर और भी दृढ हुआ हूं, तर्क और भी पैना हुआ है। अपनी बात को औरों तक पहुंचाने के लिए और इसी अभिव्यक्ति के लिए ब्लॉग तथा सोशल मीडिया को माध्यम बनाना और लिखना शुरू किया, जो अब जारी है। जारी रहेगा। ‘Youth Ki Awaaz’ ने मेरे पहले लेख “सार्वजनिक जगहों पर दूध पिलाती मां का स्तन देखकर पितृसत्ता क्यों डर जाती है?” को अहमियत देते हुए अपने पोर्टल पर डाला, तो फिर और उत्साह बढ़ गया। मुझे पहला ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला जहां पर आपको आपके विचार के लिए कोई जज नहीं करता, कठघरे में खड़ा नहीं करता, बल्कि आपको अपनी सोच और विचार को अभिव्यक्त करने का मौका देता है।
इसी उत्साह ने मुझे, 8 दिनों में 4 लेख लिखने को प्रेरित किया। ‘Youth Ki Awaaz’ ने मुझे कुछ अन्य साथियों के साथ ‘यूजर ऑफ़ द वीक’ में भी शामिल कर लिया। ..तो अब हौसले से लबरेज, अपनी लेखनी को और भी धार देता हुआ, हर उस बात पर खुलकर बात करने को तैयार हूँ, जिसे करने से पहले डरता था। खाशकर, धर्म, जाति-भेद, जेंडर, पितृसत्ता, अंधभक्ति और सामाजिक कुरीतियों पर। ‘Youth Ki Awaaz’ द्वारा मुझे दिए अतिरिक्त हौसले के लिए और उनके इस नायाब प्रयास के लिए, बहुत-बहुत सलाम!
लिखने को प्रेरित करने के लिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!
(आभार: लेख मूल रूप से यूथ की आवाज के लिए लिखा गया है।)

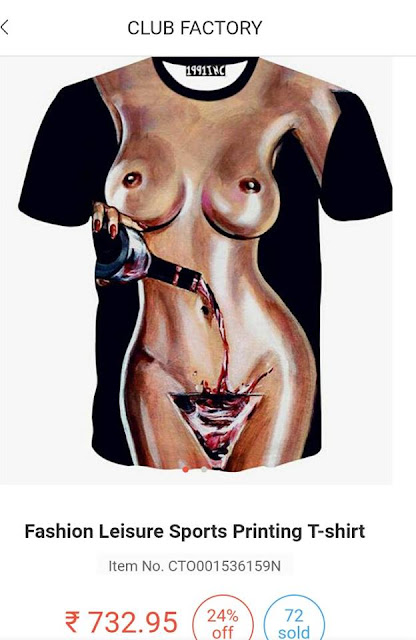
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thank you for comment