गिजूभाई बधेका: जिन्होंने बच्चों का शैक्षिक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा-कृष्ण प्रताप सिंह
बच्चे स्कूल जाने से हीलाहवाली करने के बजाय उत्साह व उल्लास के साथ वहां जाएं और जीवनोपयोगी शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए गिजूभाई ने कई क्रांतिकारी प्रयोग किए.
 |
| गिजूभाई बधेका (फोटो साभार: विकीपीडिया)
महात्मा गांधी के गुजरात में उन्हीं जैसे एक और ‘तपस्वी’ हुए हैं-गिजूभाई बधेका. 15 नवंबर, 1885 को सौराष्ट्र के चीतल में उनका जन्म हुआ तो मां-बाप ने नाम रखा था-गिरिजा शंकर भगमानजी.
अभी मैट्रिक परीक्षा ही पास की थी कि रोजी-रोटी की फिक्र उन्हें अफ्रीका खींच ले गई. तीन साल बाद वहां से लौटे तो जानें कैसे उन पर अधूरी रह गई अपनी शिक्षा पूरी करने की धुन सवार हो गई.
फिर तो उन्होंने मुंबई जाकर, और तो और, कानून तक की पढ़ाई की. यह और बात है कि लेकिन महात्मा गांधी की ही तरह वकालत की पारी को लंबी नहीं खींच सके और सक्रियताओं का नया क्षेत्र चुन लिया, जो बच्चों की शिक्षा का था.
दरअसल, उन दिनों देश में बच्चों की शिक्षा के प्रति जो उपदेशात्मक, अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक व दकियानूस रवैया अपनाया जाता था और जिस कारण अपनी किस्तों में हुई पढ़ाई के दौरान खुद गिजूभाई को भी नाना प्रकार की विडंबनाएं झेलनी पड़ी थीं, उससे वे अंदर-बाहर दोनों बेहद आहत महसूस करते और चाहते थे कि जिन स्थितियों ने उन्हें इतना सताया, वे किसी और बच्चे को किंचित भी न सता सकें.
इसके लिए उन्होंने उनके उन्मूलन की दिशा में प्रयत्न शुरू किए तो उनमें ऐसे रम गये कि अनेक बच्चे उन्हें ‘मूंछों वाली मां’ कहने लगे, जबकि बड़े ‘बच्चों का गांधी’ या ‘बाल शिक्षा का सूत्रधार’.
जानकारों के अनुसार 1920 से लेकर 1939 तक उन्होंने बच्चों की शिक्षा का परीक्षा के साथ चला आ रहा पुराना गठजोड़ खत्म करने और उसे अक्षरों के साथ दृश्य-श्रव्य माध्यमों से जोड़ने के लिए ठीक वैसी ही तपस्या व संघर्ष किये जैसे महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए.
इसीलिए कई जानकार कहते हैं कि स्कूलों में स्नेह और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का शैक्षिक स्वतंत्रता संगाम तो सच्चे अर्थों में गिजूभाई बधेका ने ही लड़ा.
बताते हैं कि उनके चित्त में बच्चों का यह शैक्षिक स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने का विचार तब आया, जब अपने बेटे के दाखिले के लिए उपयुक्त विद्यालय की उनकी तलाश किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी. यानी एक भी विद्यालय उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया.
वे अपने खुद के अनुभव से जानते थे कि सख्त शिक्षकों व कठोर दंड की व्यवस्था के कारण विद्यालयों के प्रति बच्चों में फैले भय व अरुचि को दूर किए बिना बाल शिक्षा का उद्धार होने वाला नहीं है. इसलिए उन्होंने इसी बिंदु पर सबसे ज्यादा जोर दिया.
बच्चे स्कूल जाने से हीलाहवाली करने के बजाय उत्साह व उल्लास के साथ वहां जायें और जीवनोपयोगी शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए गिजूभाई ने कई क्रांतिकारी प्रयोग किए.
इन्हीं प्रयोगों में से एक था, मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति को ग्रामीण भारत के सीमित आर्थिक साधनों के अनुरूप ढालकर इस्तेमाल में लाना. इस अनूठी पहल के तहत उन्होंने 1920 में भावनगर में दक्षिणमूर्ति बालमंदिर नाम से जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय यानी नर्सरी स्कूल खोला, उसमें पहली बार दो ढाई वर्ष के बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता खुला. इससे पहले उन्हें छह सात साल के होने पर स्कूल भेजा जाता था.
प्रसंगवश, दक्षिणमूर्ति बालमंदिर में उबाऊ पाठ्यपुस्तकों और तोतारटंत से पूरा परहेज बरता जाता था. बच्चों में सीखने की ललक पैदा कर क्रमिक विकास लाने के लक्ष्य को समर्पित इस विद्यालय में कहानियों, लोककथाओं, नाटकों, गायन, नृत्य और चित्रों की मार्फत उन्हें इस तरह शिक्षित करने पर जोर था कि वे खेल-खेल में ही बहुत कुछ सीख जायें और सीखने की परंपरा से चली आ रही त्रासद प्रक्रिया से उनका साक्षात्कार न हो.
यह जानना दिलचस्प है कि बच्चों को विचारों, कल्पनाओं और संस्कारों के स्तर पर मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस स्कूल में जिन नाटकों को मंचित किया जाता था, उनमें अन्य कलाकारों के अलावा गिजूभाई खुद भी अभिनय करते थे.
इतना ही नहीं, बाल कलाकारों को उनके संवाद रटाये नहीं समझाये जाते थे और वे उनमें अपनी रचनात्मक मेधा के प्रयोग के लिए आजाद थे. अपनी धुन के धनी गिजूभाई शिक्षा को उपदेशात्मक रूप देने के कट्टर विरोधी थे.
अपने इसी विचार के आधार पर उन्होंने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने वाली महात्मा गांधी की बालपोथी को अनुपयुक्त पाया तो उसकी आलोचना से भी नहीं चूके. बाद में उनकी आलोचना को सही ठहराते हुए गांधी जी ने स्वयं इस बालपोथी के प्रकाशन व वितरण का काम रोक दिया.
गिजूभाई भाषा व व्याकरण को अलग-अलग नहीं बल्कि एक साथ पढ़ाने के हिमायती थे और शिक्षा के दृश्य-श्रव्य माध्यमों पर अक्षरों के गैरजरूरी वर्चस्व से नाराज होते थे.
दक्षिणमूर्ति बालमंदिर के संचालन के क्रम में जल्दी ही उन्होंने समझ लिया था कि जैसी शिक्षा वे बच्चों को देना चाहते हैं, उसे उन तक पहुचाना प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या के अभाव में संभव नहीं है.
इसलिए 1925 में उन्होंने दक्षिणमूर्ति अध्यापक मंदिर भी स्थापित किया, जिसमें छह सौ से ज्यादा अध्यापकों को प्रशिक्षित कर उनकी सेवाओं का सदुपयोग सुनिश्चित किया गया.
बच्चों के लिए जरूरी साहित्य के सृजन का काम पिछड़े नहीं, इसके लिए गिजूभाई ने खुद भी बड़ा सृजनात्मक योगदान दिया. उन्होंने बाल कहानियां व बालगीत तो रचे ही, यात्राओं व साहसिक अभियानों पर भी पुस्तकें लिखीं.
उनकी लिखी पुस्तकों की कुल संख्या एक सौ बताई जाती है. उनकी लंबी कहानी ‘दिवास्वप्न’ को बालशिक्षा के नए रूप के संविधान और बाल साहित्य के सिरमौर जैसा आदर प्राप्त है. इसमें वे व्यवस्था देते हैं कि बच्चों के विद्यालयों को बालश्रम शोषण शिविर जैसा बनाने से बाज आना और शारीरिक प्रताड़ना से मुक्त कराना चाहिए.
जिस साल उन्होंने दक्षिणमूर्ति अध्यापक मंदिर स्थापित किया, उसी साल शीरामती ताराबाई मोदक के साथ मिलकर गुजराती में ‘शिक्षण पत्रिका’ का प्रकाशन किया. शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव के पक्ष में चेतना पैदा करने और जन सामान्य को अपनी शिक्षा पद्धति की जानकारी देने के लिए उन्होंने भावनगर और अहमदाबाद में दो सम्मेलन भी आयोजित किए.
1936 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में कुछ सहयोगियों से मतभेदों के कारण उन्हें दक्षिणमूर्ति संस्था छोडकर राजकोट में एक अध्यापक मंदिर बनाना पड़ा. लेकिन उम्र ने उनको उसे फलता-फूलता देखने का अवसर नहीं दिया.
23 जून, 1939 को वे मृत्यु से अपना युद्ध हार गए और हमने एक अपनी तरह का अनूठा बालशिक्षा शास्त्री खो दिया.
(आभार: द वायर हिंदी, लेख मूल रूप से द वायर हिंदी के लिए लिखा गया है, लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और फ़ैज़ाबाद में रहते हैं.)
|

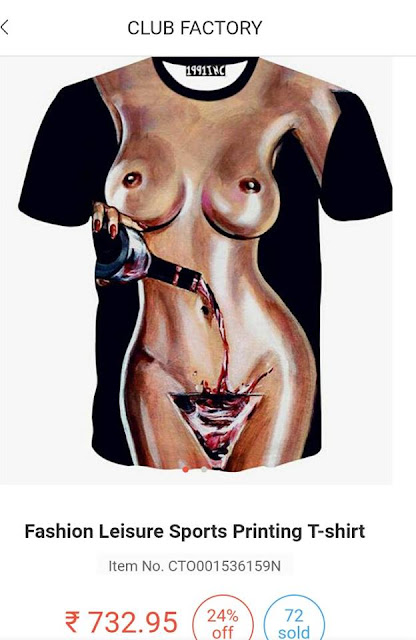
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thank you for comment