उम्मीद जगाता, धर्म और जाति का खाली कॉलम वाला केरल का शिक्षा मॉडल- प्रत्युष प्रशांत
देश की कुल आबादी में कम ही लोग ऐसे होंगे, जो किसी भी आवेदन में राष्ट्रीयता, धर्म, जाति और लिंग के कॉलम से नहीं गुज़रे हों। कमोबेश हर शिक्षित संस्थान के आवेदन फॉर्म में इन कॉलमों का होना और इसको भरना लाज़मी होता है, आप इससे बचकर या इसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
परंतु, केरल ने अपने राज्य के स्कूलों में बच्चों को पहली से बारहवीं तक के उनके नामांकन में धर्म और जाति के कॉलमों से कई सालों से मुक्त कर रखा है। वहां के बच्चे हरेक सत्र में नामंकन के दौरान अपने धर्म और जाति का कोई उल्लेख नहीं करते हैं। इस बार सारे एडमिशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए होने की वजह से यह आंकड़ें सामने आए हैं। पिछले दिनों केरल विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सी रवीन्द्रनाथ द्वारा दिये गये लिखित जवाब के बाद यह बात स्पष्ट हुई।
भारतीय संविधान की धारा 51, जो नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को लेकर है तथा जो वैज्ञानिक चिंतन, मानवता, सुधार और खोजबीन की प्रवृत्ति विकसित करने पर ज़ोर देती है, उस संदर्भ में यह समाचार महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक शिक्षा के निदेशक के वी मोहनकुमर बताते हैं
कोर्ट के आदेशों के आधार पर, छात्रों को उनकी जाति या धर्म का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, नतीजतन स्कूल अब किसी को भी अपनी जाति का उल्लेख करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए इन छात्रों ने इसका उल्लेख नहीं किया है। जब वह बड़े वयस्क बन जाए तो खुद के विकल्प को चुन सकते है।
किसी भी समाज को धर्म और जातिहीन समाज बनाने के लिए यह एक बेमिसाल कदम है। समाज में जाति और धर्म आधारित असमानता नहीं रहे, इसके लिए हमें उस प्रक्रिया को बदलना होगा जो जातिगत या धार्मिक अंतर को सामाजिक विभेद में बदल देती हैं। निश्चय ही केरल राज्य में बच्चों को पहली से बारहवीं तक के उनके नामंकन में धर्म और जाति के कॉलमों से मुक्त रखने की परिकल्पना में समाज की भी अपनी महत्ती भूमिका होगी।
इस प्रक्रिया में अहम भूमिका परिवार और घर की तो होगी ही, पर शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। देश के कई राज्यों से बराबर मिड-डे मील योजना में वंचित समाज के बच्चों के साथ असमान्य व्यवहार की खबरें आती रहती हैं, वहां भी इसतरह के प्रयास मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। धर्म और जातिविहीन समाज बनाने के लिए इस तरह के प्रभावी कदम को पूरे भारत में लागू किया जा सकता है या नहीं, यह एक यक्ष प्रश्न है।
महात्मा फूले, पेरियार, बाबा साहब और डॉ. लोहिया ने समतामूलक समाज के लिए और जातिवाद पर प्रहार कर भारतीय लोकतंत्र को, संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से मज़बूत आधार देने की कोशिश की। परंतु, भारतीय लोकतंत्र के साथ-साथ समाज को मज़बूत सामाजिक आधार देने के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक-सांस्कृतिक कोशिशों से जातिवाद और धार्मिक मान्यताओं या मिथकों पर कठोर प्रहार किया जाए।
मौजूदा दौर में जब एक तरफ विज्ञान के क्षेत्र में रोज़ नये-नये आविष्कारों ने तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठाया है, वहीं दूसरी तरफ हम अपने आस-पास तमाम आस्थाओं के चलते सहज सुलभ होती विभिन्न असहिष्णुताओं या विवादों का हिंसक तांडव भी देख रहे हैं। इस दौर में माता-पिता, अभिभावकों की धार्मिक और जातीय आस्था के संदर्भ में एक नई तरह की अंतरक्रिया अधिक उपयुक्त दिखती है, क्योंकि बचपन में किसी किताब में पढ़ाया गया था कि “परिवार ही जीवन की प्राथमिक पाठशाला हैं।”
बालमन पर होने वाले धार्मिक प्रभावों के परिणामों पर विस्तार से लिखने वाले ब्रिटिश विद्वान रिचर्ड डांकिंस सुझाव देते हुए लिखते हैं “क्या हम “इसाई बच्चा/बच्ची” कहने के स्थान पर “इसाई माता-पिता की संतान” के तौर पर बच्चे/बच्ची को संबोधित नहीं कर सकते, ताकि बच्चा यह जान सके कि आंखों की रंग की तरह आस्था को अपने आप विरासत से ग्रहण नहीं किया जाता।” जाति की नैतिकता और धर्म की आस्था में डूबे हुए समाज को आने वाले भविष्य के लिए इसपर सोचने की ज़रूरत है।


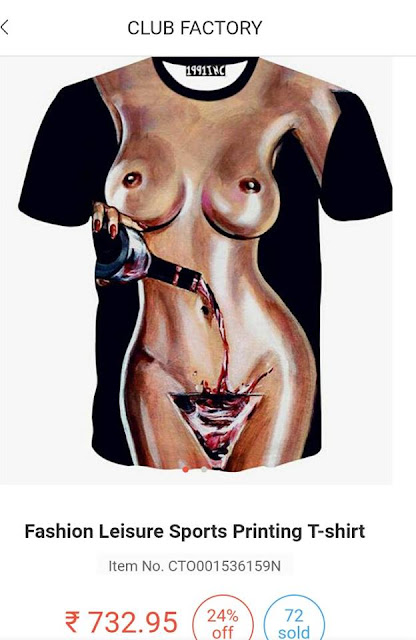
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thank you for comment