स्वप्न और संघर्षों की फंतासी बुनती है लघु उपन्यास “प्रोस्तोर”
साईबर स्पेस पर मित्र बने, एम.एम.चंद्रा से स्टेट्स पर अपने-अपने तर्कों की तलवार से सहमति-असमति भर का रिश्ता था, कभी मुलाकात करने का मौका नहीं मिला, एक दिन उन्होंने अपने लघु उपन्यास भेजने की इच्छा चैट बाक्स में जाहिर की और कल उनका लघु उपन्यास “प्रोस्तोर” कल कुरियर से मिला। आदत के अनुसार इस लघु उपन्यास का आरंभ और अंत की लाईन पढ़ना हूं, फिर आरंभ और अंत का पन्ना। उपन्यास पढ़ना है या नहीं रूचि मेरी चाय के चुस्कियों के तरह धीरे-धीरे पैदा होती है।
शुरूआत की लाईन “गुलमोहर के पेड़ सड़क के दोनों ओर फूलों से लदे खड़े हैं। उनके टूटे हुए फूल रास्ते पर ऐसे बिछे हैं जैसे किसी शाही व्यक्ति के स्वागत में फूलों की वर्षा की गयी हो। यही वो फूंल हैं जो बिना किसी भेदभाव के सबका स्वागत करते हैं। यही वो फूल हैं जो मंदिर की शोभा भी बढ़ाते हैं और पैरों से कुचले भी हाते है।” और अंत “मुझे विश्वास है हम जरूर मिलेंगे अपने सपनों के लिए…..नई दुनिया बनाने के लिए…नई दुनिया रचने के लिए” पढ़ा। बैकंग्राऊड में FM पर “छोटी सी बात” फिल्म का गाना बज रहा था “ये दिन क्या आए,लगे फूल हंसने”। जाहिर है, गुलमोहर के फूल और सपनों को जिंदा रखने संघर्ष मुझे हिप्नोटाइज कर चूका था।
इतना कुछ काफी था इस लघु उपन्यास को पूरा पढ़ने के लिए, बस जम गया “प्रोस्तोर” को पढ़ने। उपन्यास एक धांगा मिल के पास बस्ती के बसने आबाद होने, उजड़ने और अंत में जीवन की तमाम उम्मीदों के नेस्तनाबूत होने पर उसमें भी चिंगारी के बंचे होने की कहानी बहुत ही सरल और सहज भाषा में बांधे हुए रखती है। शायद इसलिए उपन्यास के अंतिम खंड में, मेट्रो स्टेशन के सीढ़ियों पर जड़ हो गया, इसे खत्म करने के लिए।
शाम तक कमरे पर लौटते हुए उपन्यास के पात्रों के सपने, संघर्ष, 90 के बाद के दिनों से अभी तक के राजनीतिक और सामाजिक हालातों का एक रोजनामचा दिमागी उथल-पुथल मचा रहा था। शायद इस लिए भी क्योंकि जिस कालखंण्ड का चित्रण लेखन ने इस उपन्यास में किया है वो ख़ुद मेरे भी दुनियावी होने का दौर रहा है। कहीं न कहीं मैंने भी सपनों और संघर्षों के कठोर यथार्थ को अपने चश्में से देखा-समझा है।
एम.एम.चंद्रा “प्रोस्तोर” एक साथ कई सवालों की रेस शुरू कर देती है कमोबेश हर सवाल एक-दूसरे के साथ भाग-दौड़ में अव्वल आने के जद्दोजहद में है। इन सवालों के भाग-दौड़ का संबंध उन्पयास के पात्रों के साथ धीरे-धीरे बनता चला जाता है और तमाम पात्रों का संघर्ष अपने सपनों के साथ उभरते हुए संजीव होने लगता है इस उम्मीद में कि “सब कुछ ठीक हो जाएगा।” अचछे दिन के चर्चित जुमले की तरह।
उपन्यास अपने साथ मज़दूर आंदोलन की राजनीति, ठेकेदारी प्रथा, मज़दूरों की बीमारियां, शिक्षा का बुरा हाल, हिंदु-मुस्लिम विवाद और उदारीकरण इन सारे सवालों को पात्रों के साथ लेकर चलता है और इनके सामाजिक संबंधों के ताने-बाने को पात्रों के सपनों से भी जोड़ता है और हकीकत का आईना भी दिखाता है।
सपना भी कैसा? एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी और बच्चों को काम नहीं करना पड़ेगा और यथार्थ यह कि जैसे नई आर्थिक नीति ने मज़दूरों को ठेकादारी का ढ़ेला खाने को मज़बूर कर दिया, उसी तरह प्राइवेट स्कूल ने सरकारी स्कूलों को तबाह कर दिया।
उपन्यास इसलिए भी अंत तक बांधे रखती है क्योंकि “प्रोस्तोर” अतीत के सवालों के साथ-साथ मौजूदा समय के सवालों के साथ भी संघर्ष करती है। उपन्यास के पात्र मास्टरजी बताते है कि “मंदिर मस्जिद का मुद्दा जानबूझकर छेड़ा गया है ताकि जनता के मूलभूत मुद्दों और लड़ाई से लोगों का ध्यान हटाया जा सके।” मानो बतया जा रहा हो कि समय कोई भी रहा हो जनता कल भी निरीह थी वह आज भी है।
पाकेट बुक्स के साइज में उपलब्ध लघु उपन्यास "प्रोस्तोर" का कैनवास इसलिए बहुत बड़ा है, इसके पात्र प्रेम अंतिरजना पर कोई बात नहीं करते है। उपन्यास मेरे लिए इसलिए अधिक मजेदार होने लगती है क्योकि वह संघर्षों के साथ स्वपन देखने का साहस हमेशा करती है और अंत में विश्वास संघर्ष का शखनांद करते हुए विदा लेती है।
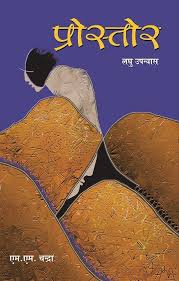

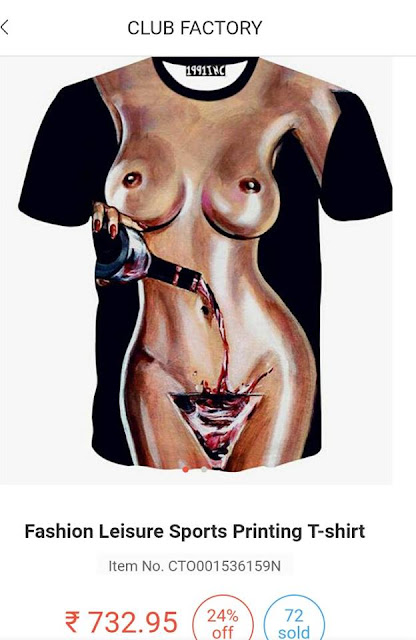
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thank you for comment