भारतीय राष्ट्रवादी विमर्श में महिलाओं के प्रश्न -प्रत्युष प्रशांत
।
वर्तमान समय में भारतीय
राष्ट्रवाद पर बहस अपने अतीत के बहसों के तरह ही कई खेमों में बंटी हुई दिखती है।
मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक परिदॄश्य में राष्ट्रवाद एक तरह के सामाजिक सिद्धांत के
रूप में स्थापित दिखता है, जिसके व्यावहारिक रूप में विरोधाभास भी मौजूद है। एक
तरफ राष्ट्रवाद की परिकल्पना आत्मपरिपूर्ति की रही है जो स्वतंत्रता और समानता
जैसे सार्वभौम मूल्यों के भविष्य का वायदा स्थापित करता है। वही दूसरी तरफ, यह
यथास्थिति के अवधारणा का सिद्ध फर्मूला भी है जो पहले दिखाये काल्पनिक यर्थाथ के
सपने को पूरा नहीं कर पाता है। आजादी के संघर्ष में और उसके बाद भी सार्वभौम
मूल्यों(स्वतंत्रता,समानता और बधुंत्व) का प्रलोभन दिखाकर राष्ट्रवादी मूल्यों का
बखूबी दोहन किया जाता रहा है। स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद जिस रूप में सामाजिक जीवन
में मौजूद है वह राष्ट्र के नाम पर संगठित करने की राजनीति में या राष्ट्रप्रेम के
भाव में व्यापक समतावादी संदर्भ को हाशिये पर ले जाता है।
इस बात में कोई
संदेह नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में राष्ट्रवाद ने निर्णायक
भूमिका अदा की। परंतु, राष्ट्रवादी बहसों ने अपने समाज में मौजूद भेदभाव, शोषण और
अन्याय को कभी विमर्श का विषय भी नहीं बनाया। गोपाल गुरू, बाबा साहब आंबेडकर के उद्दरण से राष्ट्रवाद के सीमाओं के
बारे में बताते है “राष्ट्रवाद को अगर ऊंचाई
हासिल करनी है तो स्वराज के साथ सुराज को भी जोड़ना होगा। सुराज के आधार पर समता से
संपन्न और सभी किस्म की शोषणमुक्त इंसानियत से परिपूर्ण समाज-व्यवस्था होगी।”[1] राष्ट्रवादी
आंदोलनों के दौर में भारतीय समाज में मौजूद जाति और लिंग आधारित व्यवस्था में,
महिलाएं शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में, पुरुष के इच्छा, वर्चस्व व
आकांक्षाओं के जकड़न में अधीनस्थत/शोषित स्थिति में रहने के लिए नियतिबद्ध थी।
जिसके कारण महिलाओं के लिए राष्ट्र/राष्ट्रवाद वह भावबोध पैदा नहीं कर सका जैसा की पुरुषों के संदर्भ में होता है। राष्ट्रवाद और जेंडर विडंबनाएं को नोट करते हुए, तमार मेयर लिखती
है कि “राष्ट्रीय अहं पुरुष अहं और स्त्री अहं दोनों के साथ गुंथा होता है और इसे
जेंडर तथा यौनिकता से अलग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रवाद एक जुबान बनकर यौन
नियंत्रण और दमन को जायज ठहराता है और पुरुष पराक्रम को अभिव्यक्त कर उसका
इस्तेमाल करता है।”[2] राष्ट्रवाद के
बहसों का यही वर्चस्वशाली स्वरूप उसके मूल्यांकन की मांग करता है। क्योंकि मुख्यधारा
के राष्ट्रवाद ने एक ऐसे समरस राष्ट्र के अस्तित्व की मान्यता को स्थापित करता है
जो राष्ट्रवाद की बहुआयामी पक्ष को नजरअंदाज करता है। जिसके कारण असहमति के स्वरों
जैसे स्त्रियों, दलितों या वंचित तबकों के दावे हाशिये पर सिमट गये, जबकि वह मौजूद
थे। राष्ट्रवादी बहसों ने समाज के जिन सवालों को हाशिये पर रखने का काम किया उसका
संबंध महिलाओं के सामाजिक स्थितियों या निजी/सार्वजनिक जीवन से भी जुड़ता है। औपनिवेशिक
सत्ता के विरोध में महिलाएं किस प्रकार राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल थी और
राष्ट्र–राज्य के साथ अपने संबंध को देख रही थी? और राष्ट्रवादी आंदोलनों में सहभागी महिलाएं किन महिलाओं के
स्वरों का प्रतिनिधित्व कर रही थी? महिलाओं व उनसे संबंधित मुद्दों के संबंध में
राष्ट्रवादी विचार की दृष्टि और समाज सुधार के प्रति उनके राजनीतिक उद्देश्यों की
समीक्षा भी इस शॊध आलेख का मुख्य उद्देश्य है।
।।
राष्ट्रवाद की आधुनिक व्याख्या राष्ट्रवाद को नैसर्गिक न मानकर,
समकालीन इतिहास की परिणति के रूप में देखती है। परंतु, उन्नसवी और बीसवी सदी के
प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रवाद वह बहुआयामी विमर्श है जिसमें भारतीय समाज के मध्य
बैचेनी से भरा हुआ द्दंद भी है। भारतीय राष्ट्रवादी विमर्श में मुख्य बिंदु यह है
कि यह उपनिवेशवाद के विरोधी संघर्ष में एक ऐसी साझी जनभावना के रूप में विकसित या
लामबंद हुई, जिसने जन समुदाय को भूगोल, भाषा, सभ्यता, जातीयता, धर्म और समान
राजसत्ता के आधार पर संगठित किया। राष्ट्रवाद ने एक राष्ट्र की इस अवधारणा के रूप
में वजूद में आया जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में आने वाली सभी आर्थिक,
राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने की कोशिश किया। राष्ट्रवादी
आंदोलनों के प्रकृति का विश्लेषण करते हुए, रोजा लग्जमबर्ग कहती है कि “राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रवाद खाली बर्तन हैं जिसमें हर
युग और हर देश के वर्ग-संबंध अपने विशिष्ट सारतत्व उड़ेल देते है।”[3] भारतीय संदर्भ
में राष्ट्र के इस भावना में परराष्ट्रों के पराभाव का भाव भी शामिल था। इसके
साथ-साथ जातीय राष्ट्रवाद ने जाति के वर्चस्व को राष्ट्रवाद के रूप में विकसित
किया तो धार्मिक राष्ट्रवाद ने धर्म को राष्ट्रीय गर्व का विषय बनाया। इसी तरह
भाषा, सांस्कृति, इतिहास के आधार पर भी राष्ट्रवाद का विकास दिखता है। इस क्रम में
राष्ट्रवाद को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय मिथकों,
राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्र के मूर्ति जैसे उपकरण के रूप जुड़ते
चलते गये। राज्यसत्ता ने राष्ट्रीय सम्मान को राष्ट्रवाद के विमर्श से जोड़ दिया।
राष्ट्रवाद की
बहसों को औपनिवेशिक/साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और उपाश्रित (subalitem) परिपेक्ष्य में देखा और समझा जाता रहा है जिसके अपने
सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ
है। इन नजरियों ने राष्ट्रीय आंदोलनों को अलग-अलग
तरीकों से पहचाना और विश्लेषण किया। राष्ट्रवादी विमर्शों में
औपनिवेशिक/साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन आंदोलन के रूप
में स्वीकार नहीं किया। उनका विश्वास था कि साम्राज्यवाद, सभ्यता तथा सामाजिक
सुधारों के साथ भारत आया। इस आधार पर औपनिवेशिक/साम्राज्यवादी इतिहासकार इस तथ्य
को खारिज करते हैं कि औपनिवेशिक शक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा
आर्थिक शोषण के विरुद्ध भारत में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह इतिहासकारों
का समूह यह नहीं मानता हैं कि भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था। इसके अनुसार
भारत में धर्म, जातियों, समुदायों और अलग-अलग हितों समूह के आधार पर एक समुच्चय का
निमार्ण किया और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल अपने-अपने निजी हितों के पूर्ति के लिए
किया। यह कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक/साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद भारतीय जनता और
उपनिवेशवाद के बीच आपसी हितों और अंतविरोधों के द्दंद्दों के बीच फंसा हुआ था।
इतिहासलेखन
परंपरा में राष्ट्रवादी लेखकों ने भारत में राष्ट्रवाद की पहचान एक प्रमुख सत्ता
के रूप में की जिसने स्वतंत्रता और स्वाधीनता के विचार को गतिशीलता प्रदान की। भारतीय
राष्ट्रवाद की व्याख्या में राष्ट्रवादी लेखकों ने औपनिवेशिक शासन के शोषण को आधार
बनाकर, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में देखने का प्रयास किया।
राष्ट्रवाद की इस विचारधारा ने भारतीय राष्ट्र को एक रूप में जोड़ने और भारतीय जनता
के रूप में उनकी पहचान बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यह एहसास
कि देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां देश के लोगों को एक दूसरे के
करीब ला रही है, लेकिन राष्ट्रीय लक्ष्य पाने के लिए लोगों में राजनीतिक चेतना का
विकास करना होगा। इसलिए जरूरी है कि लोगों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की
भावना को बढ़ावा दिया जाए।”[4] राष्ट्रवाद के इसी विकास पर चर्चा करते हुए
ए.आर.देसाई लिखते है कि “राष्ट्र ऐतिहासिक तौर पर
विकसित होती है; यह भाषा, भूक्षेत्र, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक एकता में
परिलक्षित मनोवैज्ञानिक अस्तित्व का
स्थित, निश्चित संयोग है।”[5]
इतिहासलेखन में
मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद के वर्गीय चरित्र का विश्लेषण करने
में कार्ल मार्क्स के मूलभूत विचारों को अपना आधार बनाया। मार्क्सवादी इतिहासकारों
ने राष्ट्रवाद के उस परिकल्पना प्रश्नांकित जो भाषिक, भौगोलिक, सामाजिक, वर्गीय,
जातीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अथवा पूंजीवादी हितों के आधार लामबंद होते है। इस
विचारधारा के अनुसार राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवाद के उस पूंजीवाद का
परिणाम है, जो औधोगिक क्रांति के कारण विकसित हुई और जिसने शोषणकारी व्यवस्था को
जन्म दिया। राष्ट्रवादी आंदलोन के वर्गीय चरित्र की आलोचना करते हुए इस विचारधारा
ने किसानों तथा अन्य वर्गों के शोषण के सवाल को हाशिये से केंद्र में लाने का
प्रयास किया। परंतु मार्क्सवादी राष्ट्रवाद की मुख्य आलोचना उपनिवेश विरोधी मुख्य
अंतर्विरोध और भारतीय समाज के भीतर के गौण अंतर्विरोधों के विश्लेषण में एक-दूसरे
से तालमेल नहीं बैठा पाने के कारण है। अन्य राष्ट्रवादी विचारधारों के तरह
मार्क्सवादी राष्ट्रवाद का नजरिया वर्ग की अवधारणा और उसके अनुसार व्यवहार के चलते
मुक्ति की अन्य प्रभावशाली अवधारणाओं को हाशिये पर रखा।
सबलटर्न
विचारधारा ने इतिहासशास्त्र में भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन में सबलटर्न
विचारधारा ने हाशिये पर डाल दिए गये लोगों के विमर्श को केंद्र में लाने का प्रयास
किया। इतिहास को नीचे से देखने का यह नजरिया शोषण के आधार और प्रकृति को लेकर
मार्क्सवादी व्याख्या से भिन्न था। सबलटर्न इतिहासकारों ने अपने ऐतिहासिक विवेचना
में ‘चेतना’ को केंद्रीय
स्थान दिया। जिसके आधार पर इतिहास लेखन में असहमति दर्ज की। सबलटर्न विचारधारा औपनिवेशिक
सत्ता के अधीनस्थ किसान विद्रोहियों की ऐतिहासिक पड़ताल इतिहासलेखन में अभिजन और
निम्नवर्ग के दोहरे विभाजन को विमर्श के सतह पर लाने का प्रयास करता है। एजाज अहमद
बताते है “इतिहासशास्त्र के इस स्कूल ने पुनर्जागरण,
तर्कवाद और इतिहासवाद की सर्वाधिक आलोचना के साथ जोड़ दिया।”[6] स्पष्ट शब्दों
में सबलटर्न विचारधारा इतिहासकारों एक ऐसा मंच रहा जिसकी परिधि निम्न जाति,
आदिवासी, किसान विद्रोह से मध्यवर्गीय विचारधारा में राष्ट्रवाद, राजनीतिक मिथकों
के महत्व, जाति और जेंडर की अस्मिता की व्याख्याओं का विस्तार करता है।
राष्ट्रवाद पर
मौजूद अवधारणाएं इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि राष्ट्रवाद एक तनावग्रस्त स्थिति
रही है। राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के कोशिश में यह कहा जा सकता है कि
राष्ट्रवाद वह विचार या भावना है जो स्वयं के जरिये अपना खुद का इतिहास बनाती है। हम
राष्ट्र को कैसे देखते है? कहां से देखते है और किस तरह से देखते है? यह ज्यादा
महत्वपूर्ण है।
।।।
विचार के
अवधारणात्मक स्वरूप में राष्ट्रवाद समावेशी विचारधारा के विरूद्ध खड़ी दिखती है जो
राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक सीमाओं पर आधारित राजनीति को गतिशीलता प्रदान करती
है। यह राष्ट्रीय पहचान सभी समुदायों को समानता नहीं दे पाता, क्योंकि इन
राष्ट्रीय पहचान का निर्माण सामाजिक और सांस्कृतिक वर्चस्व के आधार पर होता है। राष्ट्रवाद
की यही प्रकृति महिलाओं के अस्मिता के साथ जुड़ते समय काफी द्दंद्दात्मक हो जाती है
क्योंकि किसी भी राष्ट्र में ऐतिहासिक रूप
से जब महिलाएं समान स्थिति में ही नहीं रही है तो वह
राष्ट्रवादी कैसे हो सकती है? महिलाओं के राष्ट्रवादी विश्लेषण में इस तथ्य को
समझना आवश्यक है कि किस प्रकार महिलाओं की जेंडरीकृत
भूमिकाएं राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान परिभाषित एंव स्थापित हो रही थी, किसप्रकार औपनिवेशविरोधी राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाएं शामिल हो
रही थी ? और महिलाएं
उपनिवेश विरोधी आंदोलनों में राष्ट्र-राज्य के साथ अपनी भूमिकाओं को किसप्रकार देखती
या समझती हैं ?
भारतीय राष्ट्रवादी विमर्श में, राष्ट्रीय संस्कृति की आकृति,
स्वरूप तथा पहचान की व्याख्या की कोशिश में महिलाओं के प्रश्न ने केंद्रीय महत्व
प्राप्त हुआ। परंतु, उपनिवेशी शासकों और राष्ट्रवादी वर्गों के बीच महिलाओं के
प्रश्न काफी उलझा हुआ भी था। आधुनिकता व प्रगति का विषय बन जाने के कारण नई स्त्री
की छवि के तलाश में उपनिवेशी शासकों और राष्ट्रवादी वर्ग के समाजसुधारक सामाजिक
कुरतियों को मिटाना चाहते थे लेकिन समाज के मौजूद ढांचे और उसमें महिलाओं की
(कमतर) हैसियत की कोई आलोचना नहीं करते थे। समाज-सुधारकों ने सामाजिक सुधार के लिए
स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन भी किया। औपनिवेशिक
शासन काल में भारतीय समाज-सुधारकों की मानसिकता स्पष्ट करते हुए शेखर बंधोपाध्याय
बताते है कि “भारत के मध्यवर्गीय पुरूष विक्टोरियाई आदर्श वाली सहचरी के सपने देखते थे।
बंगाल में शिक्षित भद्रमहिला प्रबुद्ध हिंदू पत्नी बनाना तो दूर, इस शिक्षा ने
स्त्रियों को सुपत्नी और सुमाता की आदर्शमंडित घरेलू भूमिकाओं से सीमाबद्ध कर
दिया।”[7] राष्ट्रवादी समाज-सुधारकों ने नई शिक्षित स्त्री को
सार्वजनिक जीवन की गतिविधियों में भाग लेने की छूट अवश्य दी। परंतु, घरेलू कामकाज
अब भी उसका प्रमुख कार्यक्षेत्र था। इसतरह महिलाएं मुक्ति के प्रश्न राष्ट्रवादी
पुरुषों के समाधान में फंस गई और स्त्री समानता, स्वतंत्रता जैसे विषय पीछे ढकेल
दिए गये।
इसके साथ-साथ राष्ट्रवादी राजनीति ने महिलाओं के राष्ट्रीय
पहचान के निमार्ण में महिला की छवि को सांस्कृतिक परंपराओं में खोजा और उन्हीं के
आधार पर निर्मित किया। अपनी स्वाभाविक जरूरत के लिए राष्ट्रवाद ने स्त्रीत्व के
परंपरागत आदर्श छवि को केंद्रीय महत्व दिया। राष्ट्रवादी चेतना के तहत स्त्री
चेतना का विकास आरंभ से ही पितृसत्ता के लिंगीय अनुशासन के अधीन रहा और सार्वजनिक
क्षेत्र में स्त्रियों की भूमिका सार्वजनिक अनुशासन के नाम पर पहले से तय थी। समाज
सुधारकों ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, पर उसकी सीमाबंदी भी भरपूर तरीकों से
की। महिलाओं के लिए मिथकीय चरित्र के चयन के आधार और उसके प्रस्तुतीकरण को इतिहास
की आधी-अधूरी समझ के तर्क को उमा चक्रवति प्रश्नाकिंत करते हुए लिखती है कि “राष्ट्रवादी यह
बताते है कि वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति उच्च थी, जबकि ऐसा करते हुए वह सिर्फ
आर्य महिलाओं (उच्च जाति की अभिजनवादी महिलाओं) की बात कर रहे होते हैं क्योंकि
वैदिक काल में ही गैर आर्य महिलाएं (वैदिक दासी) उस समय भी शोषित की जाती थी।
सिर्फ गार्गी और मैत्रेयी जैसी कुछ उच्च जाति की महिलाओं के प्रस्तुतीकरण से सभी
महिलाओं की स्थिति का सही अंदाजा लगाना निरर्थक हैं। यह इतिहास को गलत रूप में
प्रस्तुत करने का तरीका मात्र है, जिससे यह तथ्य छिपाया जा सके कि उस समय भी
महिलाएं समाज से गायब थी।”[8] राष्ट्रवादी आंदोलनों में
राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करने के इस तरह के प्रयास यह सिद्ध करता है कि
राष्ट्रवादी विमर्श ने महिलाओं के प्रश्न को संकुचित क्षेत्रों तक सीमित रखने का
प्रयास किया।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौर में महिलाओं के
प्रश्न और नई स्त्री के रूप में उसका समाधान मोटे तौर पर एक वर्ग आधारित भी प्रतीत
होती है। अनेक महिलाएं इस देशकाल में औधोगिक श्रमिक जमात का हिस्सा थी जो अपने
वेतन और काम के हालात के सिलसिले में उपनिवेशवाद के तहत पनप रहे पूंजीवाद और
पितृसत्ता से संघर्ष कर रही थी। यह राष्ट्रवादी विमर्श की सीमाओं के तरह इशारा
करती है कि राष्ट्रवादी विमर्श की बहस केवल मध्यवर्गीय स्त्रियां ही थी जो घर की
चौहद्दी में बंद थी और जिंन्हें गृहिणी या भद्र महिला के दायरे में रखा जा सकता
है। परंतु, स्त्री की दुनिया केवल घर के चौहद्दी तक सीमित नहीं हो सकती। इसमें
विधवा महिलाएं भी हो सकती है, वेश्याएं भी हो सकती हैं, परिवार में प्रतिभाशाली
बहनें, माताएं या पत्नियां भी हो सकती है, वृद्ध पतियों की बालिका-वधू हो सकती
हैं, सब्जी और फेरे लगानी वाली महिलाएं भी हो सकती है, घरों में काम करने वाली
महरी या दाई हो सकती है, खेतों में काम करने वाली महिलाएं हो सकती है। चारु गुप्ता औपनिवेशिक काल के
राष्ट्रवादी चिंतन की सीमाओं को पहचानते हुए लिखती है कि “औपनिवेशिक भारत के
खास संदर्भ में जाति, दलित पहचान, लैंगिक विचारधारा और पौरुष के आत्मविवेचन नहीं
दिखती हैं।”[9] स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी
बहसों में निष्काषित और उपेक्षित भावों से भरे समूह के रूप में महिलाओं के प्रश्न
राष्ट्रवादी राजनीति के लोकतांत्रिक होने की सीमाओं पर इशारा करती है और राष्ट्रवादी
बहसों में इन महिलाओं के प्रश्न की अनदेखी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
औपनिवेशिक दौर
में समाज-सुधारकों व राष्ट्रवादियों द्दारा महिलाओं के महिमामंडन व स्त्रियों पर
लगाये गये प्रतिबंधो से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रवाद भी एक पौरूषपूर्ण विचार
है जिसमें पुरुषों को महत्व दिया और महिलाओं के लिए नई पितृसत्ता का निमार्ण किया।
इसने स्त्री मुक्ति के प्रश्नों को सार्वजनिक धरातल पर हल करने बजाय परिवार के
दायरे में सीमित करने की कोशिश की।
भारतीय
राष्ट्रवादी आंनदोलन में महिलाओं की सहभागिता और संघर्ष के प्रश्न पर अभय कुमार
दुबे बताते है कि “एक तरफ महिलाओं ने
राष्ट्रवाद की उपनिवेशवाद विरोधी राजनीतिक दावेवारी में अपना स्वर मिलाना स्वीकार
किया, क्योंकि उसके माध्यम से उनके लिए एक नया दरवाजा खुल रहा था। दूसरी तरफ,
उन्होंने राष्ट्रवाद की मर्दवादी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और जकड़बंदियों को
चुनौतियां देते हुए राष्ट्रवादी एजेण्डे में नारीवादी ऐजेंसी के जरिये पितृसत्ता
विरोधी पहलुओं का समावेश करने का यत्न किया।“[10]
वास्तव में राष्ट्रवादी आंदोलन के दौर में महिलाएं उस उत्पीड़क संरचनाओं के
विरुद्ध लड़ रही थी- उन नैतिक संहिताओं के दायरे में जो बुर्जुआ राष्ट्रवादियों और
समाज-सुधारकों द्दारा निर्धारित किए गये थे। परंतु, इन निर्धारित सीमाओं ने भारतीय
स्त्री को मुक्ति के रास्ते पर चलने की प्रेरणाएं भी उपलब्ध कराई। राधा कुमार ‘स्त्री संघर्ष के इतिहास में’ चर्चा करती है कि “1890 के दशक के दौरान
स्त्रियों ने राष्ट्रवादी आंदोलनों एंव संगठनों में भाग लेना शुरू किया। हालांकि
काफी हद तक स्त्रियों को अपने आसपास मंडराते पुरुषों के विरोध का सामना भी करना
पड़ा। कांग्रेस के अधिवेशन में महिला प्रतिनिधियों को भाग लेने की अनुमति मिली।
परंतु, उन्हें बोलने या प्रस्तावों पर वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया।
कांग्रेस अधिवेशन में महिलाएं अपनी जिन समस्याओं को उठाना चाहती थी उसमें
वेश्यावृत्ति पहला प्रमुख मुद्दा था।”[11]
इस दशक में उत्पन्न नई शक्तियों ने
स्त्री चेतना के विकास को गतिशीलता प्रदान की, जिसने राष्ट्रवादी संघर्षों में
स्त्रियों को खुद भी भूमिका निभाने का अवसर मिला।
20वीं सदी के आरंभ में राष्ट्रवाद के बढ़ते उभार ने, स्त्रीत्व
के मातृत्व रूप को राष्ट्रीय राजनीति में लोगों को संगठित करने के एक सशक्त माध्यम
के रूप में स्थापित करना आरंभ कर दिया। जानकी नैयर बताती है कि “राष्ट्रवाद के अंतर्गत स्त्री के मातृत्व रूप को सर्वोच्च
महत्व दिये जाने से, न केवल स्त्री की पारिवारिक पोषक की भूमिका को दृढ़ता मिली,
वरन स्त्रीत्व का सार के रूप में आत्मत्याग, नि:स्वार्थ सेवा, सहिष्णुता व
आत्मबदिलान के गुणों को सर्वोच्च प्रतिष्ठा दी गई। यह विचार राष्ट्रवादी विचारधारा
में इतना प्रभावशाली बनकर उभरा कि तात्कालीन प्रमुख राष्ट्रवादी नेता सुरेन्द्रनाथ
बनर्जी ने सभी भारतीयों से आह्वान करते हुए कहा कि- मित्रों आप चाहे किसी भी जाति
या वर्ण के हों आइये हम सब अपने मतभेदों को भुलाकर मातृत्व धर्म के झंडे तले एकजुट
हो जाए।”[12]
राष्ट्रवादी आंदोलनों में मातृकेंद्रित वाग्मिता ने महिलाओं की सहभागिता को
तेज किया। किस-किस वर्ग के महिलाओं को राष्ट्रवादी आंदोलनों में सहभागिता मिली यह
एक विचारणीय प्रश्न है? इन गतिविधियों ने महिला अधिकारों को न केवल राष्ट्रवाद से
जोड़ा बल्कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की मांग को राष्ट्रवादी
दलीलों के जरिए बचाव भी किया। इन्द्राणी चटर्जी लिखती है कि “कुछ स्त्रियों ने यह विचार व्यक्त करना शुरु कर दिया कि
स्त्रियां अगर आजाद होना चाहती हैं तो उन्हें पुरुषों के साथ संघर्ष के लिए तैयार
रहना चाहिए। दोनों लिगों में बराबरी की जहां तक बात है यह स्वयं समानता के
सिद्दांत पर आधारित है न कि किसी की दया पर।”[13]
20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिला सहभागिता दो भिन्न सिद्धांतों के
साथ संघर्षरत दिखता या प्रतीत होता है। पहला, यह कि चूंकि स्त्रियां मां के तौर पर
अधिक उपयोगी है इसलिए उनके अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए और दूसरा यह कि चूंकि
महिलाओं की जरूरतें, इच्छाएं तथा क्षमताएं पुरुषों के समान हैं इसलिए वे समान
अधिकारों की हकदार है। राष्ट्रवादी आंदोलन में स्त्री सक्रियता की बढ़ती
राजनैतिक-सामाजिक चेतना का प्रत्यक्ष प्रमाण, राज्य के विरूद्ध स्त्रियों को एक
समूह के रूप में संगठित होना भी है। महिलाएं अपने सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और
राजनीतिक अधीनीकरण से आजादी पाने के लिए न केवल राष्ट्रीय मुक्ति बल्कि सामाजिक रूपांतरण
के मोर्चे पर भी सक्रिय रूप से सहभागी थी। राष्ट्रवादी आंदोलनों ने महिला सहभागिता
का उपयोग निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर को तोड़े बिना ही किया। इन आंदोलनों ने
भारत की महिलाओं में पहली बार प्रजातंत्र, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को
जाना-समझा। जिससे महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई परंतु, इन आंदोलनों ने
कभी भी लैगिंक समनता जैसे मुद्दे नहीं उठाए और ना ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था को
चुनौती दी।
स्पष्ट है कि लैंगिक असमानता, राष्ट्रवाद का अविभाज्य हिस्सा है। औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के लिए भारत में हुए
राष्ट्रीय संघर्षों ने स्त्री शिक्षा और महिलाओं के सहभागिता को अपने-अपने तरीके
से परिभाषित किया, लैंगिक समानता और स्वतंत्रता के काल्पनिक यथार्थ को जीवित रखा। भारत
में महिलाओं ने स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई
परंतु, बाद में उन्हें घर की चहारदीवारी के अंदर धकेल दिया गया और उनसे यह अपेक्षा की जाने लगी कि पारंपरिक
सीमाओं का पालन करें जो सामाजिक नैतिकता के लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती हो।
महिलाओं का
राष्ट्र-राज्य और राष्ट्रवाद के संबंधों की पहचान के क्रम में, हम पाते है कि
व्यक्ति जिस समाज या राज्य का सदस्य है, के साथ संबंध अनिवार्य रूप से उसकी
सामाजिक संरचना द्दारा निर्धारित होता है। इस सामाजिक स्थिति में के आधार पर
दुर्गा दास बसु बताते है कि “सामाजिक संरचना में
असमानता की स्थिति में स्त्रियों का के लिए राष्ट्र/राष्ट्रवाद वह बोध पैदा नहीं
कर सकता था और न उस तरह से अर्थित हो सकता था जैसा कि वो पुरुषों के संदर्भ में था।”[14] राष्ट्र को
अक्सर राजनीतिक शक्ति के प्रस्तुतीकरण से जोड़कर देखा जाता रहा है बल्कि राष्ट्रीय
शक्ति का प्रतिनिधित्व भी जेंडर विभेद पर निर्भर करता है। जिसके कारण पुरुष की हताशा
और आकांक्षा राष्ट्र से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। वर्जिनिया वुल्फ दूसरे विश्व
युद्ध के समय में राष्ट्र-राज्य के साथ महिलाओं के संबंधों की बारीकियों की पड़ताल
करते हुए लिखती है कि “महिलाएं अपने विषय में
देशभक्ति के अर्थ का विश्लेषण करेगी तो अपने अतीत में लिंग और वर्ग का लेखा-जोखा
लेगी। वह इस बात पर विचार करेंगी कि स्त्री आज कितनी जमीन, संपत्ति और धन-धान्य की
स्वामिनी है। वह कहेगी, इतिहास के ज्यादातर काल में मुझे सिर्फ दास मानता आया है;
इसने मुझे शिक्षा या मालिकाने में किस प्रकार की हिस्सेदारी से बेदखल रखा.....असल
में एक औरत के तौर पर मेरा कोई देश नहीं। एक औरत के तौर पर मैं कोई देश भी नहीं चाहती।
एक औरत के रूप में पूरी दुनिया मेरा देश है।”[15]
वुल्फ महिलाओं और राष्ट्र
के संबंधों के बारे में महिलाओं की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के आधार पर अभिव्यक्त
करती है। जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि महिलाएं राष्ट्र और नागरिकता के बीच
पेडुलम वाली स्थिति में है।
जबकि, राष्ट्र और
महिलाओं के संबंध को राष्ट्र की संरचना व महिलाओं के पुनरूत्पाद के संदर्भ में
उसके उपयोग को रेखांकित करते है। नीरा
युवाल-डेविस और फ्लोरा एन्थियास राष्ट्र और महिलाओं के संबंध को पांच प्रमुख
बिंदुओं से चिन्हित करती है- “(1) राष्ट्रीय समूह के सदस्यों की जैविक प्रजननकर्ता के रूप में, (2) राष्ट्रीय समूहों की सीमाओं
के प्रजननकर्ता के रूप में(यौन एंव वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध के जरिए) (3) राष्ट्रीय संस्कृति के
सक्रिय प्रचारक व उत्पादक के रूप में (4) राष्ट्रीय विभेद के प्रतीकात्मक संकेतक के रूप में (5) राष्ट्रीय संघर्षों में
सक्रिय हिस्सेदारी के रूप में। ये सभी प्रवृत्तियां विशेष ऐतिहासिक क्षणों में
स्त्री को विशेष प्रकार से निर्मित करते हैं।”[16] नीरा युवाल-डेविस और फ्लोरा
एन्थियास का यह विश्लेषण जेंडर, राष्ट्र और यौनिकता के विषय ध्यान केंद्रित कराते
है। साथ ही यह इशारा करते है कि राष्ट्र को फायदा पहुंचाने, उन्हें प्राप्त करने
या उनपर नियंत्रण करने का सवाल हमेशा ही जेंडर से प्रभावित होता है। कई नारीवादी
शोधों ने उजागर किया है कि राष्ट्रीय परियोजानाओं में मर्द और औरतें अलग-अलग ढंग
से शरीक होते है। इस तरह के अधिकांश कार्यों ने राष्ट्र की रचना के बरक्स औरतों के
हाशियाकरण के सवाल पर ही अपने जो केंद्रित किया है।* इसे किसी राष्ट्र की
कुछ राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से भी समझा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय
परियोजना में महिलाओं की केंद्रीयता के सवाल पर अपना ध्यान केंद्रीत करती है। जहां
राष्ट्रीय संदर्भ में स्त्रीत्व का निर्माण पुरुषों, राष्ट्र और बाद में राज्य की
नीतियों के बरक्स होता है। आमतौर पर स्त्रीत्व को राष्ट्र के निमार्ण में सहयोग
देनेवाले एक साधन के रूप में पेश किया जाता है, यह सहयोग प्रतीकात्मक, नैतिक और
जैविक पुनरुत्पादन के रूप में सामने आता है। भारतीय संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण
के मामले में ‘हम
दो हमारे दो’,
का नारा या स्लोगन ’गर्भनिरोध स्वीकारकर्ता’ जैसे परियोजनाओं को उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है। जहां राष्ट्र को
सहेज कर रखने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर रखी जाती है, कभी-कभी इसके लिए धार्मिक
तर्क-विमर्श भी पेश किए जाते है। इस तरह महिलाओं को अक्सर राष्ट्र के प्रति
कर्तव्यों को पूरा करने के रूप में देखा जाता है।
जहां एक तरफ महिलाओं का प्रजननात्मक/पुनरुत्पादनात्मक
क्षमता को सामूहिक राष्ट्रीय ढांचे के लिए महत्वपूर्ण रहे है। वही दूसरी राष्ट्र
के लिए शरीर भी एक महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है। एक राष्ट्र की महिलाएं उसकी सरहद
का प्रतीक बन जाती है। भारतीय उपमहाद्दीप के बंटवारे के समय महिलाओं के साथ हुए
हिंसक घटनाएं इसका उदाहरण बन सकती है। टकराव के स्थितियों में महिलाओं के साथ
यौनिक हिंसा राष्ट्र की इज्जत लूटने का हथियार बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई
लड़की दूसरे देश में बलात्कार के कारण गर्भवती हो जाती है और अपने देश में गर्भपात
पर प्रतिबंध के कारण दूसरे देश की जाने की योजना करती है तो लड़की के गर्भ से भरा
शरीर राष्ट्र की आदर्श छवि का समानार्थी बन जाता है। महिलाओं का बलात्कार
राष्ट्रीय सरहदों, राष्ट्रीय स्वायत्ता और राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघनों के
रूप में राष्ट्र पर हमला का प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल होते है। इस तरह
महिलाओं के शरीरों पर किए जाने वाले हमले राष्ट्र के पुरुषों पर हमले का प्रतीक बन
जाते है।
स्पष्ट है कि महिलाएं स्वयं व्यावहारिकता के धरालत पर
राष्ट्र–राज्य के साथ खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है परंतु, राष्ट्र, जेंडर और
उसकी जैविक स्थिति एक-दूसरे को इस तरह गढ़ने का प्रयास करती है कि उसकी भूमिका
परिभाषित होती है। भारत में ‘भारत माता’ का प्रतीक इस्तेमाल किया गया है। इसमें भारत के भौगोलिक नक्शे पर एक औरत
शरीर को दिखाया जाता है। ऐसा शरीर जिसे चाहा जाता है, जिस पर कब्जा बरकरार रखा जा
सकता है और जिसकी रक्षा करना जरूरी है। राष्ट्र इस तरह महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ
होता है और राष्ट्र के काम के रूप में जेंडर आधारित बंटवारा भी होता है। महिलाएं
प्रतीक के रूप में राष्ट्र को पुनरुत्पादित करती है और पुरुष राष्ट्र की रक्षा
करते हैं, उसका बचाव करते हैं और उसके लिए बदला भी लेते है।
हालांकि राष्ट्र
की पहचान कभी स्थिर नहीं होती है बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिपेक्ष्य
में वह हमेशा बनने की प्रक्रिया में रहती/होती है। इसलिए कभी हो सकता है कि
राष्ट्रीय संदर्भ में पुरुषों के साथ मर्दागनी और स्त्रियों के साथ औरतानापन का
सीधा संबंध बदल जाए। यह तब हो सकता है, जब या तो राष्ट्र का तर्क विमर्श बदल जाए
या जेंडर और यौनिकता का।
संदर्भ :
[1] गोपाल गुरू, दलित बौद्धिकता और सांस्कृतिक
दीवारें, सं अभय कुमार दुबे, आधुनिकता के आइने में दलित, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली,2014 पेज न०-141
[2]
तमार मेयर, जेंडर आयरनीज आंफ नेशनलिज्म: सेटिंग
द स्टेज का हिंदी अनुवाद, रंजीत, राष्ट्रवाद की जेंडर विडंबनाएं, निरंतर प्रकाशन,
नई दिल्ली,2011, पेज न०-172|
[3] ए.आर.देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन
प्रवृत्तियां, ग्रंथशिल्पी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016, पेज न०-80।
[4] विपन चंद्र, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली
विश्वविधालय, दिल्ली,2000 पेज न०- 38-41
[8] उमा चक्रवती, वाट
ऎभर हैप्न टू वैदिक दासी? ओरिएटलिजम, नेशनललिजम एंड स्क्रीप्ट फार पास्ट इन
रिकास्टिग विमन....ऎसेज इन कोलोनियल हिस्ट्री संपादन, कुमकुम संगारी एंड सुरेश
वैध्य, काली फांर वुमेन नई दिल्ली, 1989, पेज न०-28
[9] चारु गुप्ता, रूप
और अरूप, सीमा और असीम, प्रतिमान, सं.अभय कुमार दुबे, नई दिल्ली, जनवरी-जून 2013, पेज न०- 100
[10] अभय कुमार दुबे, फुटपाट पर कामसूत्र, पटरी से
उतरी हुई औरतों का यूटोपिया, राष्ट्रवाद के प्रति आख्यान, वाणी प्रकाशन, नई
दिल्ली, 2016, पेज न०- 21
[13] इंद्राणी चटर्जी का अप्रकाशित शोध प्रबंध –
बंगाली भद्र महिला-1930-34, जे एन यू- 1986 पृष्ठ 91-94
[15] साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनिता
(सं०): नारीवादी राजनीति:संघर्ष एंव मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय,
दिल्ली विश्वविधालय, दिल्ली 2001, पेज न०- 78
[16] साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनिता
(सं०): नारीवादी राजनीति:संघर्ष एंव मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय,
दिल्ली विश्वविधालय, दिल्ली 2001, पेज न०- 79.
* के. जयवर्धना, फेमिनिज्म
एंड नेशनलिज्म इन द थर्ड वर्ल्ड, लंदन: जेड,(1986)
*एन.युवाल- डेविस, जेंडर
एंड नेशन, लंदन: सेज(1997)
*एन.युवाल-डेविस व एफ.
एंनाथियांस संपादित, विमेन-नेशन-जेंडर, लंदन: मैकमिलन,(1992)



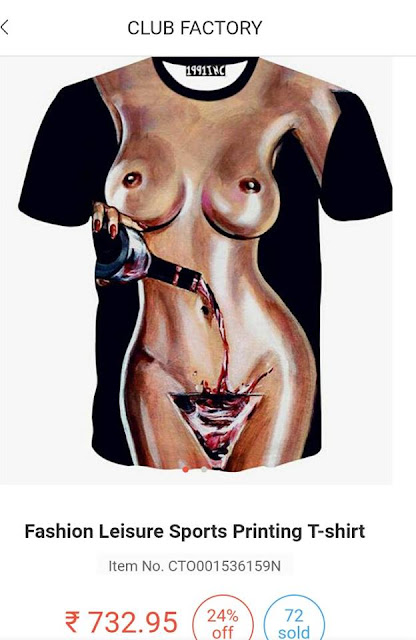
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thank you for comment