इस माहौल में विवेकानंद-पुरूषोतम अग्रवाल(आभार पुरूषोतम अग्रवाल के फेसबुक वाल से)
यह लेख राजेन्द्र माथुर द्वारा संपादित ‘नवभारत टाइम्स’ में पहले पहले छपा था, शायद 1990 या 1991 की बारह जनवरी—विवेकानंद के जन्मदिन के आस-पास। बाद में यह पुरूषोतम अग्रवाल की पहली प्रकाशित पुस्तक, ‘संस्कृति: वर्चस्व और प्रतिरोध’ ( पहला संस्करण, 1995) में संकलित किया गया।
विवेकानंद का नाम सुनते ही औसत हिंदू दिमाग में क्या तस्वीर उभरती है ? गेरुआ वस्त्रधारी, सुदर्शन, तेजस्वी संन्यासी, जिसने सितम्बर, 1893 की शिकागो धर्म-संसद में हिन्दू धर्म की महानता और मनीषा के झंडे गाड़ दिए । हिंदू होने पर शरमाने की बजाय गर्व करना सिखाया और साबित किया कि हम किसी से कम नहीं । यह तस्वीर असत्य नहीं, अर्द्धसत्य है । इसकी व्यापक लोकस्वीकृति का कारण भी असल में इसका अधूरापन ही है । अपने धर्म पर गर्व विवेकानंद अवश्य करते थे । इस गर्व का, राजनीतिक रुप से पराधीन समाज के लिए, अर्थ भी बहुत ज्यादा था । मामला राजनीतिक पराधीनता के बावजूद सांस्कृतिक स्वाभिमान बनाए रखने का था । लेकिन विवेकानंद का स्वाभिमान कूपमंडूकों के आत्मविश्वास से तो भिन्न था ही; उन पक्षियों के आक्रामक गर्व से भी अलग था, जिनकी सभा में दोपहर अँधेरी होती है ।
विवेकानंद की समग्र चिंता और गतिविधि को एक अधूरी तस्वीर तक सीमित भी तो वे ही लोग करना चाहते हैं, जो तीखे सवालों की चिलकती धूप के अस्तित्व तक से इंकार करने के इच्छुक हैं । ऐसे विवेकानंद उनके काम के हैं, जो हिंदुत्व पर गर्व करना सिखाएँ । लेकिन शूद्रराज और समाजवाद की बातें करने वाले विवेकानंद ? कर्मयोगी की नैतिकता का आधार आस्तिकता को नहीं, सामाजिक न्याय के संघर्ष को मानने वाले विवेकानंद ? वे तो झंझट पैदा करेंगे । सो, उनकी अधूरी तस्वीर को ही सब कुछ मानो । सन्यासी की तेजस्विता पर गर्व करो, लेकिन उस आत्म-संघर्ष और आलोचनात्मक विवेक से कोई वास्ता न रखो, जिससे तेजस्विता संभव हुई । विवेक की जीवंत उपस्थिति को जड़ प्रतिमा बना दो और चुनिंदा तारीखों पर फूलमाला अर्पित कर दो । यही नहीं, इस प्रतिमा के जरिए ऐसे सवालों का मुँह बंद कर दो, जिनसे विवेकानंद तब टकराए और सौ बरस बाद आज भी टकराते । परम्परा के अपहरण की इस राजनीति के शिकार विवेकानंद अकेले नहीं हैं । इसीलिए सवाल सिर्फ उनका न होकर सारी सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसे मुक्ति की दिशा में विकसित करने का है । स्वयं विवेकानंद के शब्दों में, “ताकत के बूते निर्बल की असमर्थता का फायदा उठाना धनी-मानी वर्गों का विशेषाधिकार रहा है, और इस विशेषाधिकार को ध्वस्त करना ही हर युग की नैतिकता है ।” (स्वामी विवेकानंद, 'कम्पलीट वर्क्स,' मायावती संस्करण, कलकत्ता,1950, खंड-।, पृ.434- 35.)
विवेकानंद धार्मिक व्यक्ति थे, राजनीतिक नहीं । राजनीति से उनकी विरक्ति तो “खबरदार, मुझे छूना मत” किस्म की थी । इसीलिए यह और भी ध्यान देने की बात है कि वे नैतिकता की परिभाषा विशेषाधिकार पर आधारित सत्तातंत्र के खिलाफ संघर्ष के रुप में करते हैं । तो क्या विवेकानंद धर्म का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे ? जो व्यक्ति यह कहे कि “भूखे के सामने भगवान पेश करना उसका अपमान हैं”, वह कैसा धार्मिक व्यक्ति था ? जो व्यक्ति यह पूछे कि “ धर्म को सामाजिक नियमों से क्या प्रयोजन ?” और फिर कहे कि “धर्म को कोई हक नहीं कि समाज के नियम गढ़े । उसे चाहिए कि अपनी हद में रहे ।” उसे क्योंकर धार्मिक माना जाए । ख़ास कर आज के माहौल में, जबकि ‘साधु-संत’ खुले आम राजनीतिक उठा-पटक में लगे हुए हैं । आख़िर विवेकानंद के लिए धार्मिक होने का मतबल क्या था ? उनकी कठोर सामाजिक आलोचना और सक्रियता का धार्मिकता से किस प्रकार का संबंध था ? ऐसे सवालों के संदर्भ में विवेकानंद का अर्थ समझने के लिए रामकृष्ण परमहंस को समझना अनिवार्य है । साथ ही उस परिवेश के बुनियादी सवालों को भी, जिसकी बेचैनी विवेकानंद के धर्म में वाणी पा रही थी । ऊपर से देखें तो गुरु-शिष्य दो विपरीत छोरों पर थे । विवेकानंद सुदर्शन, बलिष्ठ युवक थे, तो परमहंस क्षीणकाय । विवेकानंद अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे भद्रलोक थे, तो रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के साधारण शिक्षित पुजारी । विवेकानंद संशयवादी, बुद्धिवादी थे, तो परमहंस आस्थावान साधक ।
रामकृष्ण की साधारणता ही उनकी असाधारणता थी । वे बहुत सहज रूप से विवेकानंद (जो तब तक नरेंद्र ही थे) के सीधे सवाल का सीधा जवाब दे सकते थे, “हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है । ऐसे ही, जैसे इस वक्त तुम्हें देख रहा हूँ ।” बँधे-तुले धर्म और महीन तर्क के प्रति उदासीन निजी अनुभव पर आधारित यह आत्म-विश्वास रामकृष्ण परमहंस को मध्यकालीन भक्तों की परम्परा से जोड़ता है । रुढ़िवादी शास्त्र-धर्म के विरुद्ध जो लोकधर्म भक्तों की बानी में रचा-बसा है, रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व उसी लोकधर्म का मूर्त रुप था । साधना के नितांत निजी धरातल तक परमहंस ने हर धर्म - हिंदू, इस्लाम, ईसाई - को अपनाया था । वे संवादी सबके थे, अन्धानुयायी किसी के नहीं ।
भक्ति-संवेदना की विलक्षणता यही है कि उसने प्रेम को ही आधार माना - भक्त और भगवान का संबंध हो या मनुष्य और मनुष्य का । रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व में इस विलक्षणता ने प्रामाणिक और समकालीन अर्थ पाया तथा विवेकानंद के कर्म में व्यावहारिक विस्तार । विवेकानंद जब नारायण को दरिद्र में देखते थे, दरिद्र नारायण की सेवा को ही धर्म का सार कहते थे, तो वे उनके अपने शब्दों में “गुरु के उपदेश को जीवन में उतारने की चेष्टा” ही कर रहे थे । यह उपदेश बहुत गहरे अहसास के रुप में मिला था, युवक नरेंद्र को । जब उन्होंने निर्विकल्प समाधि पाने की साधक-सुलभ इच्छा प्रकट की, तो गुरु ने उन्हें झिड़क दिया, “धिक्कार है तुम्हें । मैं समझता था, तुम असंख्य आत्माओं के वट वृक्ष बनोगे, तुम केवल अपना स्वार्थ विचार रहे हो ।” (सत्येंद्रनाथ मजूमदार, 'विवेकानंद चरित', नागपुर, 1967, पृ.161)
परमहंस केवल नरेंद्र को धिक्कार रहे थे या उस समूचे बोध को, जिसके लिए धार्मिक होने का अर्थ था – सामाजिक यथास्थिति का सहायक होना या फिर केवल अपने मोक्ष की चिंता करना । यह धिक्कार नरेंद्र के लिए इस सच्चाई का साक्षात्कार बना कि मुक्ति अकेले को नहीं मिला करती । वे धर्म को किसी राजनीतिक प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वे निस्संदेह धर्म को जी रहे थे, लेकिन उसे नया अर्थ देते हुए । जड़ता के स्थान पर संघर्ष से धर्म को परिभाषित करते हुए । विवेकानंद उन भाग्यवानों में से नहीं थे, जिन्हें हर सवाल के तैयार जवाब मिल जाते हैं, वे उन अभागों में से भी नहीं थे, जो ऐसे रेडीमेड जवाबों को जीवन, धर्म और संस्कृति का सार मान बैठते हैं । उन्होंने न तो धर्म की प्रचलित अवधारणा स्वीकारी, न देश का चालू विचार । उन्होंने सचमुच भारत की खोज की - पूरे दो बरस देश के कोने-कोने में घूमकर उन्होंने भारतीय समाज की ताकत और कमजोरी को परखा । इस परख के ही क्रम में ही वे स्वयं को भी परख सके । जो लोग समझते हैं कि विवेकानंद को सारा बोध कन्याकुमारी के तट पर एक ही रात में हासिल हो गया, वे विवेकानंद की आंतरिक-बाह्य खोज के मर्म को समझ ही नहीं सकते ।
सन् 1891 में पैर में चक्कर लेकर निकले तेजस्वी संन्यासी विवेकानंद ने सब कुछ त्याग दिया था । सब कुछ त्याग देने का नुकसान भी होता है । वह यह कि व्यक्ति स्वयं को बहुत ऊपर समझने लगता है । ‘पवित्र’ होने के नाते उसे उन सबसे घृणा का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिन्हें वह स्वयं अपवित्र मानता हो । अप्रैल, 1891 में स्वामी विवेकानंद खेतड़ी नरेश के अतिथि थे । एक दिन ऐसा हुआ कि एक वेश्या को गाना सुनाने के लिए तलब किया गया । पवित्र संन्यासी क्षुब्ध होकर कमरे से चले गए । दुनियादार लोगों की वासना और तिरस्कार की आदी स्त्री को पवित्र सन्यासी का यह तिरस्कारपूर्ण रवैया बहुत गहरे चुभा और यह चुभन उसने व्यक्त की, सूरदास के पद में, “प्रभु मोरे अवगुन चित न धरो ।” यह विवेकानंद के पवित्रतावादी अहंकार के विगलन का क्षण था । ( रोमाँ रोलाँ, ''दि लाइफ ऑफ विवेकानंद एण्ड दि यूनिवर्सल गॉस्पेल'', कलकत्ता,1965,पृ.24-25; तथा मजूमदार, पूर्वोक्त, पृ.313-4.) उसके बाद वे कभी लांछितों, वंचितों और दलितों के प्रति सामाजिक तिरस्कार में हिस्सा नहीं बंटा सके । बल्कि इन लोगों के लिए उनकी करुणा समाज के ‘पवित्र’ भद्रलोक की कठोरतम आलोचना में व्यक्त हुई ।
विवेकानंद संभवतः अपने समय के अकेले सवर्ण कुलोत्पन्न विचारक थे, जिन्होंने भारत के उच्च वर्ग और सवर्ण समाज को बतौर सामाजिक समूह के ऐसी लगती हुई बातें कहीं, “शुद्ध आर्य रक्त का दावा करने वालो, दिन-रात प्राचीन भारत की महानता के गीत गाने वालो, जन्म से ही स्वयं को पूज्य बताने वालो, भारत के उच्च वर्गो, तुम समझते हो कि तुम जीवित हो ! अरे, तुम तो दस हजार साल पुरानी लोथ हो....तुम चलती-फिरती लाश हो....मायारुपी इस जगत् की असली माया तो तुम हो, तुम्हीं हो इस मरुस्थल की मृगतृष्णा....तुम हो गुजरे भारत के शव, अस्थि-पिंजर.....क्यों नहीं तुम हवा में विलीन हो जाते, क्यों नहीं तुम नये भारत का जन्म होने देते ?'' (स्वामी विवेकानंद, 'कम्पलीट वर्क्स' (खण्ड-7), पृ.354.)
विवेकानंद समकालीन राजनीति से दूर ही रहते थे, लेकिन उनका धर्म सामाजिक सत्ता के सवाल से लगातार टकराता था। यही कारण है कि राजनीति से कोई वास्ता न रखने वाले स्वामी विवेकानंद बार-बार राजनीतिकर्मियों के प्रेरणास्रोत बने, और यही कारण है कि शोषणकारी समाजसत्ता को बनाए रखने के इच्छुक लोग विवेकानंद को हथियाने की कोशिश बार-बार करते रहे और अब भी कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रखर सामाजिक चेतना को छद्म राष्ट्रवाद के हित में इस्तेमाल किया जा सके। इस खतरे का अहसास स्वयं विवेकानंद को था। इसीलिए उन्होंने कहा था, ''लोग देश-भक्ति की बातें करते हैं। मैं देश-भक्त हूँ, देश-भक्ति का मेरा अपना आदर्श है।.....सबसे पहली बात है, हृदय की भावना। क्या भावना आती है आपके मन में, यह देखकर कि न जाने कितने समय से देवों और ऋषियों के वंशज पशुओं-सा जीवन बिता रहे हैं ? देश पर छाया अज्ञान का अंधकार क्या आपको सचमुच बेचैन करता है? .....यह बेचैनी ही देश-भक्ति का पहला कदम है।'' (विनय रॉय द्वारा उद्धृत, 'सोशियो पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ विवेकानंद'-पी.पी.एच., नयी दिल्ली, 1983, पृ.54-55.)
गरीबी, शोषण और अज्ञान के अहसास से बेचैन होना ही देश-भक्ति का पहला प्रमाण है-पिछले सौ साल में इस कसौटी की प्रासंगिकता बढ़ी ही है। इस माहौल में, जबकि सामाजिक न्याय और देश-भक्ति को अलग-अलग किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रवाद को आक्रामकता और घृणा का पर्याय बनाया जा रहा है, तब यह कसौटी सच्ची देश-भक्ति और छद्म-राष्ट्रवाद के बीच अंतर करने के लिए बहुत जरुरी है। इन असली सवालों को राजनीतिक एजेंडा से गायब ही कर देने को जो लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, और फिर विवेकानंद के नाम की माला जपते हैं, वे सचमुच धन्य हैं और धन्य है पाखंड कर सकने की उनकी क्षमता।
विवेकानंद के समय को हम नवजागरण का समय कहते हैं। उनके परिवेश की बुनियादी समस्या यही थी। भारतीय समाज का सामाजिक-सांस्कृतिक नवजागरण। कैसे यह महादेश अपनी सांस्कृतिक पहचान फिर से प्राप्त करे? कैसे यह विराट् जनसमुदाय सामाजिक स्पंदन प्राप्त करे ? कौन-सी बाधाएँ हैं इस संभावना के रास्ते में ? कौन-सा सामाजिक तबका हटा पाएगा इन बाधाओं को ? हमारे अपने समय में भी ये सवाल अप्रासंगिक नहीं हो गए हैं, बल्कि पिछले सौ साल के अनुभवों ने कुछ नए सवाल और खड़े कर दिए हैं। विकास का अर्थ और उसकी कसौटी क्या है ? भारतीयता की पहचान क्या है ? दलितों, स्त्रियों की कोई हिस्सेदारी सामाजिक सत्तातंत्र में होनी चाहिए या नहीं ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? धर्म की मनुष्य के अंतर्जगत तथा सामाजिक जीवन में क्या भूमिका है ? हम अपने समाज की किस बात पर गर्व करें और किसके खिलाफ़ संघर्ष ? ये सवाल हमारे वर्तमान को गहरे में मथ रहे हैं। इस मंथन के माहौल में हम विवेकानंद की बैचेनी से क्या हासिल कर सकते हैं ? उनकी भावनाओं तथा विचारों की हमारे वक्त में दिशा कौन-सी हो सकती है ? परम्परा को समझने के असली सवाल ये ही हैं, और इन्हीं को भुलाने की कोशिश वे लोग करते हैं, जो विवेकानंद जैसी बेचैन मेधा को एक अधूरी तस्वीर में बदलने का अनुष्ठान कर रहे हैं।
‘कर्मयोग का आदर्श’ नामक प्रसिद्ध व्याख्यान में विवेकानंद ने कर्मयोग की विलक्षण परिभाषा की, “इस प्रकार कर्मयोग नि:स्वार्थ सद्कर्मों द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का नैतिक और धार्मिक प्रयत्न है । कर्मयोगी के लिए जरुरी नहीं कि वह किसी सिद्धांत विशेष का अनुगमन करे, आत्मा आदि के सवालों पर विचार करे। भगवान में विश्वास करना तक कर्मयोगी के लिए अपरिहार्य नहीं है।” ('सेलेक्शंस फ्रॉम स्वामी विवेकानंद', कलकत्ता, 1957, पृ.30.) यह इस कारण, क्योंकि विवेकानंद के अनुसार जीवन का मूल प्रतिमान आस्तिकता नहीं, बल्कि नैतिकता है, और नैतिकता का सार है - स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, शोषण को विशेषाधिकार मानने वाली व्यवस्था के विनाश के लिए संघर्ष।
विवेकानंद ने हिंदू समाज के संदर्भ में इन सारे सवालों पर विचार किया। दासता का स्रोत, उनके अनुसार, कूपमंडूकता और जाति प्रथा में निहित था। वे अपने समाज से सच्चा प्यार करते थे । इसलिए झूठे गर्व के जरिए लोगों को भरमाने की बजाय ताकत और कमजोरी को ठीक-ठीक पहचानने का प्रयत्न करते थे। कूपमंडूकता और जाति प्रथा के जरिए समाज की छाती पर सवार उच्च वर्ग को धिक्कारते हुए विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए बने-बनाये राष्ट्रवाद की पोटली उठा लाने के लिए नहीं दौड़ पड़ते थे। वे जानते थे कि राष्ट्र दरिद्रनारायण में निवास करता है, और उसे “जागना है - हलधर किसान के झोंपड़े से, मछुआरे की कुटिया से, नीची जातियों के बीच से...... राष्ट्र को जागना है - कारख़ानों और बाज़ारों से, जंगलों और पहाड़ों के निवासियों के बीच से। इन साधारण लोगों ने हजारों बरस अत्याचार सहे हैं, और इसी कारण उन्हें रक्तबीज जैसी विलक्षण जीवनी-शक्ति प्राप्त हो गई है ..... उन्हें आधी रोटी भी मिल जाए, तो ऐसी ऊर्जा उपजेगी उनके बीच, जो सारी दुनिया को हिलाकर रख देगी। भारत के उच्च वर्गों, अतीत के अस्थिपिंजरों । ये जनसाधारण ही हैं आने वाले भारत के भाग्यविधाता ।”( 'कम्पलीट वर्क्स', (खण्ड-7), पृ.309-10.)
इस आने वाले भारत की व्यवस्था की कल्पना विवेकानंद शूद्रराज के रूप में करते थे। शूद्र शब्द का प्रयोग भी वे केवल जातिवाचक अर्थ में नहीं, शोषित वर्ग के अर्थ में करते थे। उन्होंने उपनिवेशवाद के बारे में कहा था कि “इसके कारण समूचे के समूचे राष्ट्र शूद्र दशा में पहुंच गए हैं।” वे इतिहास को ब्राह्मण राज, क्षत्रिय राज, और अपने समकालीन समय को वैश्यकाल के रूप में देखते हुए आने वाले समय में शूद्रराज, अर्थात् दलितों, शोषितों के राज को अपरिहार्य मानते थे। विवेकानंद संभवत: पहले भारतीय थे, जिन्होने स्वयं को सामाजिक-आर्थिक अर्थ में ‘समाजवादी’ कहा, बेशक इस सावधानी के साथ कि “भले ही समाजवाद आदर्श व्यवस्था न हो, लेकिन न कुछ से तो बेहतर ही है।''
विवेकानंद का विरोधाभास यह था कि वे जनसाधारण को गैर-राजनीतिक रखना चाहते थे, जो कि संभव ही नहीं था । सामाजिक-सांस्कृतिक दासता के स्रोत पर चोट ही तो असली राजनीतिक कार्यवाही है। जो यह चोट करना चाहे, वह स्वयं राजनीति से कितना ही दूर भागे, राजनीति उसे कहां भागने देगी ? इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए कि इस वर्तमान में विवेकानंद के विचारों की दिशा क्या हो सकती है ?
विवकोनंद कवि भी थे । अपने अंतर्द्द्धों से वे कई बार कविता में ही टकराते थे । वे सच्चे धार्मिक व्यक्ति थे, सो कई बार उनके मन में नितांत वैयक्तिक साधना की इच्छा बलवती हो उठती थी। दरिद्रनारायण की सेवा के गुरुमंत्र और वैयक्तिक साधना के इस द्वंद् से विवेकानंद बार-बार टकराते दीखते हैं - कविताओं में, व्यक्तिगत पलों में, यहां तक कि सार्वजनिक लेखों, भाषणों तक में। इस सारे आत्मसंघर्ष के बाद हम उनके जीवन में अंतत: वही सच्चाई उभरती देखते हैं, जिसे रोमाँ रोलाँ ने ये शब्द दिए हैं : ''हां, विवेकानंद जैसा कवि बार-बार इस नर्क में लौटने को बाध्य है। यह उसकी नियति ही है, जीने का एकमात्र तर्क ही है- बार-बार जन्म लेना, इस नर्क की ज्वाला से संघर्ष करना, उससे झुलसते जनों में प्राण फूँकना, उन्हें बचाने के लिए स्वयं अपनी आहुति दे देना ही उसका धर्म है।'' (रोमाँ रोलाँ, 'विवेकानंद' लोकभारती, इलाहाबाद, 1993, पृ.105) 'धर्म' की इस समझ के कोण से देखें, तो विवेकानंद वहां नहीं हैं, जहां खोखले, आक्रामक 'गर्व' की टकसाल में हिंदू राष्ट्र का खोटा सिक्का ढाला जा रहा है। बल्कि वे वहां हैं, जहां उनकी कल्पना के शूद्रराज की संभावनाएँ टटोली जा रही हैं। विवेकानंद उन लोगों के साथ कैसे हो सकते हैं, जो 'इस नर्क की ज्वाला' में और ईंधन डाल रहे हैं? कैसे हो सकते हैं वे उनके साथ, जो करोड़ों वंचितों को आपस में लड़ाकर धर्म और देश-भक्ति का नाम लेने का दुस्साहस करते हैं? हमारे माहौल में दासता के स्रोत क्या हैं ? उसके नए-नए रुप कौन-से हैं ? मुक्ति की संघर्ष-यात्रा किस रास्ते चलेगी ? जो ये सवाल सच्चे मन से पूछे, विवेकानंद की परिभाषा पर खरे उतरने वाले देश-भक्त और कर्मयोगी वही हैं । ऐसे लोग विवेकानंद के प्रतिमा-पूजक हों या न हों, उनके विचारक्रम में हमराही अवश्य हैं। इस माहौल में विवेकानंद के सच्चे उत्तराधिकारी महंत, मठाधीश और राजमाताएँ नहीं, शंकर गुहा नियोगी और मेधा पाटेकर सरीखे लोग हैं। वे किसान, मजदूर, दलित, स्त्रियाँ तथा नौजवान हैं, जो शोषण-मुक्त समाज की स्थापना और मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा के लिए इस नर्क की ज्वाला से जूझ रहे हैं।


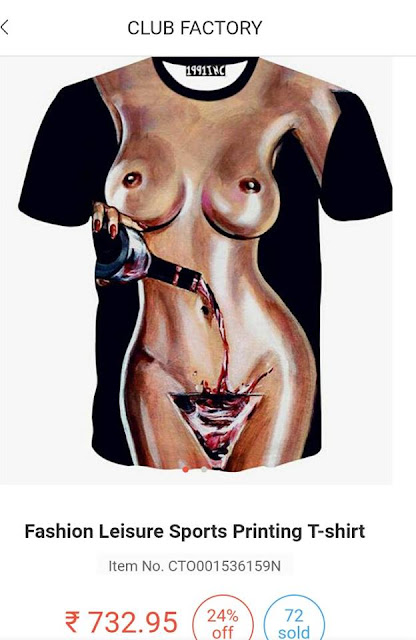
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thank you for comment