अभी तो यह अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है…. -प्रत्युष प्रशांत
विश्वविद्यालय परिसरों में लड़कियों के साथ जुल्मों-सितम की घटना कोई नई घटना नहीं है। देश में कई संस्थान हैं जिनके नियम-कायदे लड़कियों के लिए तुगलक के बेतुके फरमान के तरह है जो बैसिर-पैर के ही है। पर विश्वविद्यालय अमलदारों के पास लड़कियों के सुरक्षा की एक ऐसी छड़ी है जिसके आगे परिसरों में लड़कियां या तो विवश है या तो समय-समय पर संघर्ष करती रही है। तमाम सफल या आम महिलाओं के विश्वविद्यालय परिसर के निजी स्मरण को देखे या सुने तो यह पता चलता है कि उनको हास्टल में पहुंचने के समय निर्धारित होते थे और सुनसान सड़कों से गुजरते वक्त फब्तियों और अभद्र व्यवहारों से वो घबराई रहती थी। यह अभद्र व्यवहार मनचलों के साथ-साथ प्रशासन के लोगों के द्दारा भी होता था और इस प्रताड़ना पर शिकायत के अलावा वो कुछ नहीं कर पाती थी। यह स्थिति पहले भी आज भी है इसमें भी कोई बदलाव नहीं है और न ही तमाम विश्वविद्यालय परिसर में लड़कियों के सुरक्षा के नाम पर नियमों में। सुरक्षा के नाम पर एक दो-लाईन या अधिक या कम है पर कमोबेश एक ही तरह के है, कुछ नियम कम चटकदार है तो कुछ नियम अधिक चटकदार है, पर है सभी दायरे में बांधने वाले ही है।
इस माहौल को हास्टल में रह रही लड़कियों के “पिजड़ा तोड़” जैसे आंदोलनों से समझा जा सकता है जहां “पिजड़ा तोड़” आंदोलन की लड़कियां नियमों के साथ-साथ सामाजिक सोच में बदलाव की वकालत करती है कि समाज की सोच में आमूल-चूल बदलाव ही नया सवेरा ला सकता है। पर लड़कियों के लिए आजादी की बात नदी या तालाब के ठहरे हुए पानी में हाहदे रूपी कंकड के हलचल का इतंजार करता है और थोड़ी उथल-पुथल के बाद फिर शांत हो जाता है। विश्वविद्यालयों की हठधर्मिता और समाज की पुरातन सोच एक साथ मिलकर लड़कियों के आजादी पर हमला करते है और कुछ प्रतिरोध, मामले की संवेदनशीलता, समीतियों का गठन पर्देदारी के रूप में सामने आते है फिर खामोशी छा जाती है। विश्वविद्यालयों में छात्राओं के साथ भेदभाव और नैतिक पहरेदार के फरमान पब्लिक डोमेने में वैसे ही रहते है जैसे पहले थे।
विश्वविद्यालय ही नहीं अन्य सार्वजनिक दायरे में भी लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के सवाल के मामले में विशाखा गाईड लाईन्स मील के पत्थर कहीं जा सकती है। परंतु उसकी कार्यस्थिति उत्साह पैदा करने के जगह पर निराश ही करती है। इसकी सार्थकता इतनी भर है कि अगर सार्वजनिक स्पेस में कोई लोकतांत्रिक बांडी दिखती है तो इसका लाभ लड़कियों और महिलाओं को मिल पाता है नहीं तो वही ढांक के तीन पात का मुहावारा दोहराया जा सकता है।
जेंडर संवेदीकरण के तहों को उधेड़ने का प्रयास करे तो कई चीजें परेशान करने वाली दिखती है। आर्थिक गतिशीलता के दौर में तमाम सामाजिक और आर्थिक दबावों के आगे घुटने टेकते हुए समाज के ठेकेदारों ने यह जरूर स्वीकार कर लिया कि महिलाओं की भागीदारी हर में क्षेत्र में होना चाहिए। देश का विकास और समाज का विकास अकेले पुरुषों के वजूद से नहीं हो पायेगा। परंतु, इन दबावों ने समाज को जेंडर संवेदीकरण के लिए लोकतांत्रिक नहीं बनाया। इसलिए हर क्षेत्र में महिलाएं उपलब्धियों का मिसाल तो कायम कर रही है पर उनके जुल्मों सितम की अलग-अलग कहानियां है जिनको सुनकर सिहरन भी होती है और संघर्ष करने का हौसला भी मिलता है। अगर किताबे लिखी गई तो बेस्ट सेलर हो जाती है अगर फिल्में बनी तो करोड़ क्लब का हिस्सा बन जाती है। जाहिर है कि समाज को जेंडर संवेदीकरण के लिए अभी कोसों चलना है अभी तो ढाई घर की चाल भर चली है।
देश के तमाम नीति-निर्णाताओं ने बढ़ती कन्या हत्या, घटती कन्या शिशु-दर और लड़कियों के शिक्षा और सामाजिक स्थिति को देखते हुए कई कानून बनाए और कई नारे भी दिये। जिसमें हलिया नारा “बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ” समाज और सामाजिक संस्थाओं के अमलदारों के अपने सामंती सोच के साथ कार्य-दशाओं के कारण आलोचना के घेरे में है। स्थिति यह पैदा हो गई है कि लड़कियों को कहना पड़ा है कि “बचेगी बेटी तो पढ़ेगी बेटी”। अपनी सुरक्षा के अधिकारों पर सवाल पर जबाव मांगने पर समाज और सामाजिक संस्थाओं के अमलदारों का जो रवैया है उसको देख लड़कियां यह भी कह रही है कि “पढ़ेगी बेटी तो पीटेगी बेटी”। जाहिर है शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएं संविधान में समानता के अपने अधिकार के लिए मुखर होगी तो संघर्ष में लाठियों के दमन का सामना उनको करना पड़ेगा, पर इससे वो रूकेगी नहीं और अधिक मुखर और आत्मविश्वासी ही बनेगी। दबे जबान में जो लोग कह रहे है कि समानता के लड़ाई में उनको पुरुषों से समान ही लाठियां खानी होगी। उनके अंकगणित का हिसाब काफी कमजोर है क्योंकि जितनी यातना आधी आबादी ने झेली है वो ब्याज है उसके मूलधन के बराबर भी पुरुष समाज ने नहीं झेला है।


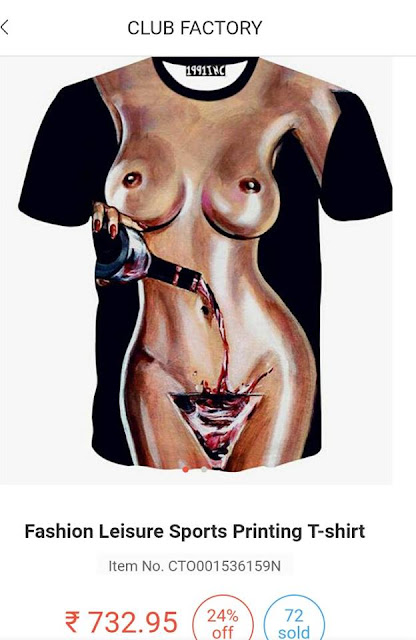
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thank you for comment